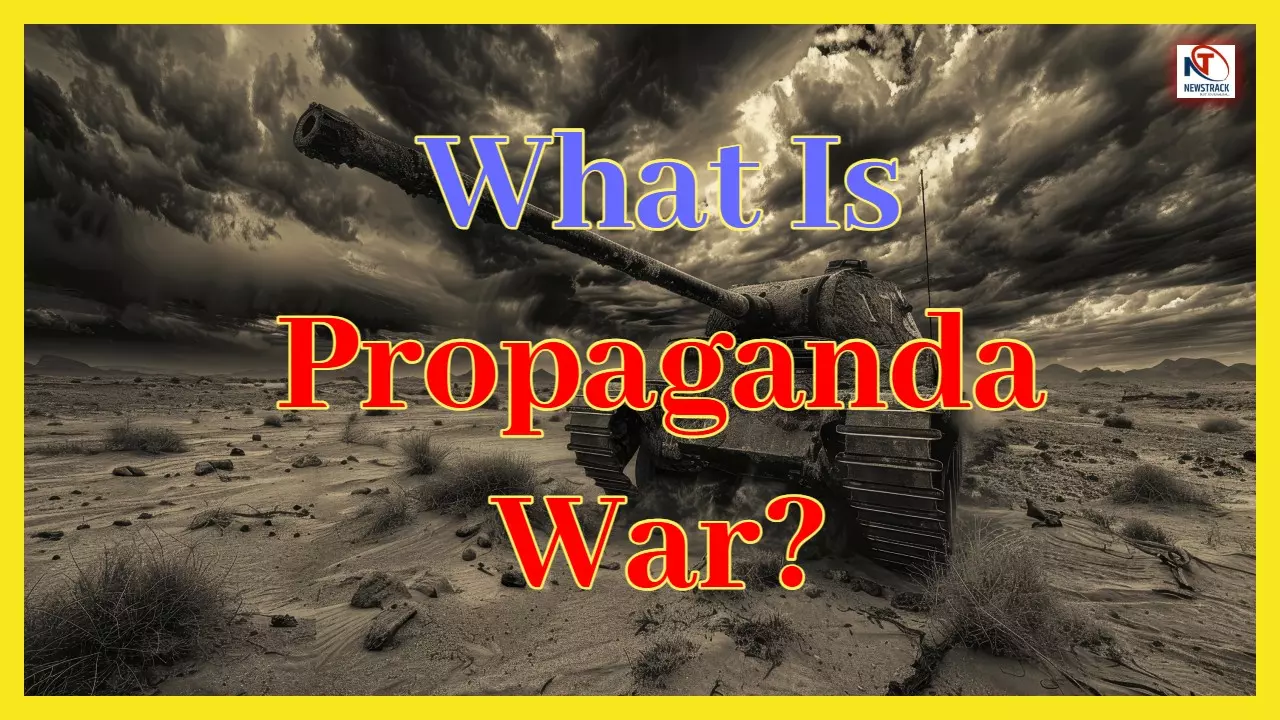TRENDING TAGS :
What is Propaganda War: जब सूचना से भड़क उठे युद्ध! आखिर क्या है प्रोपेगैंडा वॉर? जानिए इस अदृश्य हमले का सच
What is Propaganda War: यह लेख बताता है कि प्रोपेगैंडा वॉर कैसे बिना हथियार चलाए, सिर्फ सूचनाओं के ज़रिए दिमागों पर कब्ज़ा करने वाला एक खतरनाक युद्ध है।
What Is Propaganda War: युद्ध का मतलब आमतौर पर हमें बंदूकें, टैंकों, बमों और सैनिकों की भीषण लड़ाई से होता है, लेकिन 21वीं सदी ने युद्ध की एक नई और कहीं अधिक खतरनाक परिभाषा पेश की है - प्रोपेगैंडा वॉर। यह ऐसा युद्ध है जिसमें हथियार नहीं बल्कि सूचनाएं चलाई जाती हैं; बंदूकें नहीं, बल्कि टीवी चैनल, सोशल मीडिया और अखबारों की हेडलाइंस उपयोग होती हैं। दुश्मन सामने से नहीं आता, बल्कि आपके दिमाग के भीतर चुपचाप अपनी जगह बना लेता है। यह एक अदृश्य युद्ध है जहां बुलेट्स की जगह 'नैरेटिव्स' चलते हैं।
प्रोपेगैंडा वॉर क्या है?
प्रोपेगैंडा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'फैलाना' या 'प्रसार करना'। जब कोई सरकार, संगठन या समूह जनता की राय को एक खास दिशा में मोड़ने के लिए जानकारी (या गलत जानकारी) को रणनीतिक रूप से फैलाता है, तो उसे प्रोपेगैंडा कहा जाता है। और जब यह कार्य युद्ध स्तर पर और किसी देश को मानसिक रूप से कमज़ोर करने के लिए किया जाता है, तो वह बन जाता है- प्रोपेगैंडा वॉर। इस युद्ध में न तो खून बहता है, न विस्फोट होते हैं लेकिन यह समाज, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता को अंदर से तोड़ने की क्षमता रखता है।
प्रोपेगैंडा वॉर के उद्देश्य
जनमत को प्रभावित करना - प्रोपेगैंडा वॉर का मुख्य उद्देश्य जनता की सोच और राय को नियंत्रित करना होता है। इसके तहत भावनात्मक या पक्षपाती सूचनाएं फैलाकर लोगों को एक खास विचारधारा की ओर मोड़ा जाता है। चुनावों के समय फेक न्यूज़, भ्रामक वीडियो और झूठी रिपोर्टिंग से मतदाताओं को गुमराह किया जाता है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है।
राजनीतिक अस्थिरता फैलाना - प्रोपेगैंडा का एक बड़ा मकसद सरकार और विपक्ष के बीच अविश्वास बढ़ाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना होता है। अफवाहों के जरिए शांतिपूर्ण आंदोलनों को उग्र बनाना या नीतियों को गलत रूप में पेश करना इसी रणनीति का हिस्सा है। इससे जनता का भरोसा संस्थाओं से उठने लगता है।
सांस्कृतिक या धार्मिक विभाजन बढ़ाना - धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास प्रोपेगैंडा का अहम पक्ष है। लव जिहाद, धर्मांतरण, मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों पर झूठी सूचनाएं फैलाकर नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे सामाजिक एकता कमजोर होती है।
राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करना - सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के खिलाफ झूठे आरोप या नकली वीडियो फैलाकर लोगों में अविश्वास पैदा किया जाता है। इससे न केवल इन संस्थाओं का मनोबल गिरता है बल्कि आतंकी और दुश्मन ताकतों को देश को भीतर से कमजोर करने का मौका मिलता है।
भय और भ्रम का माहौल बनाना - प्रोपेगैंडा वॉर का एक उद्देश्य समाज में डर और असुरक्षा की भावना भरना भी होता है। झूठी खबरों और अफवाहों के जरिए लोगों को मानसिक रूप से कमजोर और भ्रमित किया जाता है। जिससे वे हर झूठ को सच मानने लगते हैं। यही स्थिति प्रोपेगैंडा को प्रभावी बनाती है।
प्रोपेगैंडा वॉर के प्रमुख हथियार
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स - फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि - इन प्लेटफॉर्म्स पर एडिट किए गए वीडियो, भ्रामक मीम्स और झूठी पोस्ट्स तेजी से वायरल होती हैं, जिससे आम जनता के विचार और भावनाएँ आसानी से प्रभावित हो जाती हैं। ये कंटेंट TV चैनलों और अखबारों में बहस का हिस्सा भी बन जाता है जिससे उसका असर और व्यापक हो जाता है।
फेक न्यूज़ वेबसाइट्स - इंटरनेट पर कई वेबसाइट्स असली मीडिया जैसी दिखती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य झूठी या भ्रामक खबरें फैलाना होता है। ये प्लेटफॉर्म समाज में भ्रम और वैमनस्य फैलाकर लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर कर सकते हैं।
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी (फॉरवर्डेड मैसेजेस) - आम जनता को भ्रमित करने के लिए ऑडियो और टेक्स्ट फॉरवर्ड्स, फोटो, वीडियो क्लिप्स WhatsApp पर वायरल किए जाते हैं। जिससे अफवाहें फैलती हैं और कभी-कभी दंगे या भीड़ हिंसा जैसी घटनाएँ जन्म लेती हैं।
आधिकारिक और अनाधिकारिक चैनल्स (टीवी, रेडियो, अखबार) - कई बार TV चैनलों, रेडियो या समाचार पत्रों का इस्तेमाल भी प्रोपेगैंडा फैलाने में होता है जिससे दुश्मन के नैरेटिव को मजबूती मिलती है।
साइबर बॉट्स और ट्रोल आर्मी - हज़ारों फर्जी अकाउंट और बॉट्स किसी विशेष ट्रेंड को वायरल करने, झूठ को बार-बार दोहराने और विपक्षी आवाज़ को दबाने में उपयोग किए जाते हैं। इससे जनता को भ्रमित किया जाता है और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है।
इतिहास में प्रोपेगैंडा वॉर के उदाहरण
नाज़ी जर्मनी में प्रोपेगैंडा - 1930 से 1945 तक का नाज़ी शासन प्रोपेगैंडा के सबसे भयावह प्रयोगों में से एक उदाहरण है। हिटलर की अगुवाई में नाज़ी पार्टी ने यहूदी समुदाय के खिलाफ गहरी घृणा फैलाने के लिए हर सूचना माध्यम का इस्तेमाल किया। इस अभियान का संचालन जोसेफ गोएबेल्स ने किया जिसे 'प्रोपेगैंडा मंत्री' कहा जाता था। अखबारों, रेडियो प्रसारणों और भित्ति-चित्रों (पोस्टरों) के ज़रिए यहूदी विरोधी विचारों को इस कदर समाज में भर दिया गया कि लोगों के मन में झूठ को सच मानने की प्रवृत्ति पनप गई। इसी प्रोपेगैंडा के ज़रिए 'अंतिम समाधान' जैसे नरसंहारों को सामाजिक समर्थन मिला और एक पूरी कौम को विनाश की ओर धकेल दिया गया।
शीत युद्ध का सूचना युद्ध - 1947 के बाद आरंभ हुए शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच केवल सैन्य शक्ति की नहीं बल्कि विचारधारा की भी जंग छिड़ गई। दोनों महाशक्तियों ने अपने-अपने लोकतांत्रिक या साम्यवादी मॉडलों को श्रेष्ठ दिखाने के लिए रेडियो, टीवी, फिल्मों, अखबारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सहारा लिया। इस वैचारिक संघर्ष के चलते दुनिया दो गुटों कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट में बंट गई। अमेरिका ने ‘वॉइस ऑफ अमेरिका’ जैसे प्रसारणों के माध्यम से लोकतंत्र को महिमामंडित किया जबकि सोवियत संघ ने अपनी विचारधारा को प्रचारित करने के लिए 'प्रावदा' जैसे माध्यमों का प्रयोग किया। इस काल में प्रोपेगैंडा वैश्विक राजनीति का मुख्य हथियार बन चुका था।
कश्मीर पर सूचना की जंग - कश्मीर को लेकर पाकिस्तान द्वारा चलाया गया प्रोपेगैंडा युद्ध आधुनिक समय में प्रोपेगैंडा के एक ज्वलंत उदाहरण के रूप में देखा जाता है। सोशल मीडिया, अंतरराष्ट्रीय मंचों और फर्जी समाचार नेटवर्क के माध्यम से पाकिस्तान लगातार भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश करता रहा है। फोटोशॉप की गई तस्वीरें, संदर्भ से काटे गए वीडियो और एकतरफा खबरें – इन सबका इस्तेमाल भारत को मानवाधिकार उल्लंघनकारी साबित करने के लिए किया जाता है। इन प्रयासों का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बनाना और कश्मीर मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय सहानुभूति हासिल करना है। विभिन्न रिपोर्टों और डिजिटल निगरानी एजेंसियों ने समय-समय पर इस प्रोपेगैंडा रणनीति का पर्दाफाश भी किया है।
भारत के खिलाफ प्रोपेगैंडा वॉर के उदाहरण
कश्मीर मुद्दे पर भ्रामक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग - कश्मीर को लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में कई बार ऐसी रिपोर्टिंग देखने को मिली है जो न केवल पक्षपातपूर्ण प्रतीत होती है बल्कि भारत के खिलाफ एक सोची-समझी छवि गढ़ने की कोशिश भी लगती है। कई प्रतिष्ठित संस्थानों ने अक्सर 'भारत प्रशासित कश्मीर' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में भी आतंकियों को 'आतंकी' के बजाय 'बंदूकधारी' या 'चरमपंथी' जैसे नरम शब्दों का प्रयोग इस बात को दर्शाता है कि नैरेटिव को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है। डिसइन्फो लैब और कई वैश्विक रिपोर्टों ने यह भी उजागर किया है कि पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI, अंतरराष्ट्रीय लॉबिस्ट्स के साथ मिलकर भारत-विरोधी नैरेटिव को फैलाने के लिए सुनियोजित रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। तथ्यों को अधूरा या तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने की इस प्रवृत्ति ने भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुँचाया है।
CAA-NRC विवाद और अफवाहों का सुनामी - नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और NRC को लेकर जो भ्रम फैलाया गया, वह एक संगठित प्रोपेगैंडा अभियान का हिस्सा था। सोशल मीडिया, खासकर व्हाट्सऐप और ट्विटर पर यह गलत धारणा फैलाई गई कि इन कानूनों के जरिए भारत से मुस्लिमों को निकाला जाएगा। जबकि सच्चाई यह है कि CAA केवल पड़ोसी देशों से प्रताड़ित होकर आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से संबंधित था। अफवाहों, राजनीतिक बयानों और भ्रामक मीडिया रिपोर्ट्स के कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें कुछ हिंसक भी रहे। यह पूरा घटनाक्रम दर्शाता है कि कैसे एक 'डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन' लोगों की सोच और देश की सामाजिक स्थिरता को हिला सकता है।
किसान आंदोलन में विदेशी हस्तक्षेप और नैरेटिव की लड़ाई - भारत में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान अंतरराष्ट्रीय हस्तियों जैसे पॉप स्टार रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों ने इस आंदोलन को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया। हालांकि इन हस्तियों की मंशा को लेकर मतभेद हो सकते हैं, परन्तु यह स्पष्ट है कि उनके बयानों का उपयोग भारत विरोधी नैरेटिव को मज़बूती देने के लिए किया गया। भारतीय सरकार और कई विश्लेषकों ने इस पूरे घटनाक्रम को 'संयोजित विदेशी प्रोपेगैंडा' करार दिया। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि कैसे स्थानीय मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बिना पूरे संदर्भ के उछालकर प्रोपेगैंडा का हिस्सा बनाया जा सकता है।
मॉब लिंचिंग और धार्मिक असहिष्णुता पर एकतरफा दृष्टिकोण - विदेशी मीडिया में भारत को लेकर बनाई गई एक और मजबूत नैरेटिव यह रही है कि यहां धार्मिक अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को बड़े पैमाने पर प्रमुखता से दिखाया गया लेकिन ऐसे मामलों को चयनित और एकतरफा ढंग से प्रस्तुत किया गया। कई बार जानबूझकर ऐसे विषयों को अतिरंजित रूप में सामने लाया गया ताकि भारत को 'धार्मिक असहिष्णुता' वाले देश के रूप में पेश किया जा सके। सरकारी वक्तव्यों और विश्लेषकों का कहना है कि ये रिपोर्टिंग घटनाओं के एक खास हिस्से को उजागर कर व्यापक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करती हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की छवि प्रभावित होती है।
साइबर युद्ध बनाम प्रोपेगैंडा वॉर
साइबर वॉर और प्रोपेगैंडा वॉर दोनों आधुनिक युग के प्रभावशाली हथियार हैं लेकिन इनका स्वरूप और असर अलग होता है। साइबर वॉर तकनीकी क्षेत्र में होता है जहाँ हैकिंग, डेटा चोरी और नेटवर्क ठप करने जैसी गतिविधियाँ शामिल होती हैं। इसका असर तुरंत दिखता है और इसे साइबर एक्सपर्ट्स अंजाम देते हैं। इसके विपरीत प्रोपेगैंडा वॉर मानसिक युद्ध है, जो जनता की सोच और भावनाओं को प्रभावित करता है। इसमें अफवाहें, झूठी खबरें और भ्रम फैलाकर लोगों को एक खास नैरेटिव की ओर मोड़ा जाता है। इसका असर धीमा लेकिन गहरा होता है, जो सामाजिक सोच, एकता और राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। जहाँ साइबर युद्ध सरकार और संस्थाओं पर हमला करता है वहीं प्रोपेगैंडा युद्ध आम जनमानस को निशाना बनाता है।
कैसे पहचानें कि आप प्रोपेगैंडा के शिकार हो रहे हैं?
प्रोपेगैंडा की पहचान कुछ स्पष्ट संकेतों से की जा सकती है जैसे खबर में केवल एक पक्ष दिखाया जाना, अत्यधिक भावनात्मक भाषा का प्रयोग, तथ्यों की जगह केवल राय या अफवाहें होना, संदिग्ध स्रोतों से जानकारी आना और एक ही नैरेटिव को बार-बार दोहराना। ये सभी तरीके जनता की सोच को प्रभावित करने और झूठ को सच की तरह दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
कैसे बचें इस अदृश्य युद्ध से?
फर्जी खबरों और प्रोपेगैंडा से बचने के लिए सूचना की सत्यता की जांच जरूरी है। किसी भी संदेश, वीडियो या खबर को साझा करने से पहले उसके स्रोत को जांचें और विश्वसनीय माध्यमों से ही जानकारी लें। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने से पहले सोचें और पुष्टि करें। मीडिया साक्षरता बढ़ाना भी जरूरी है ताकि लोग झूठी सूचनाओं को पहचान सकें। खासकर संवेदनशील मुद्दों पर संयम बरतें क्योंकि बिना जांच के सामग्री साझा करना सामाजिक तनाव और कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है।
Start Quiz
This Quiz helps us to increase our knowledge
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!