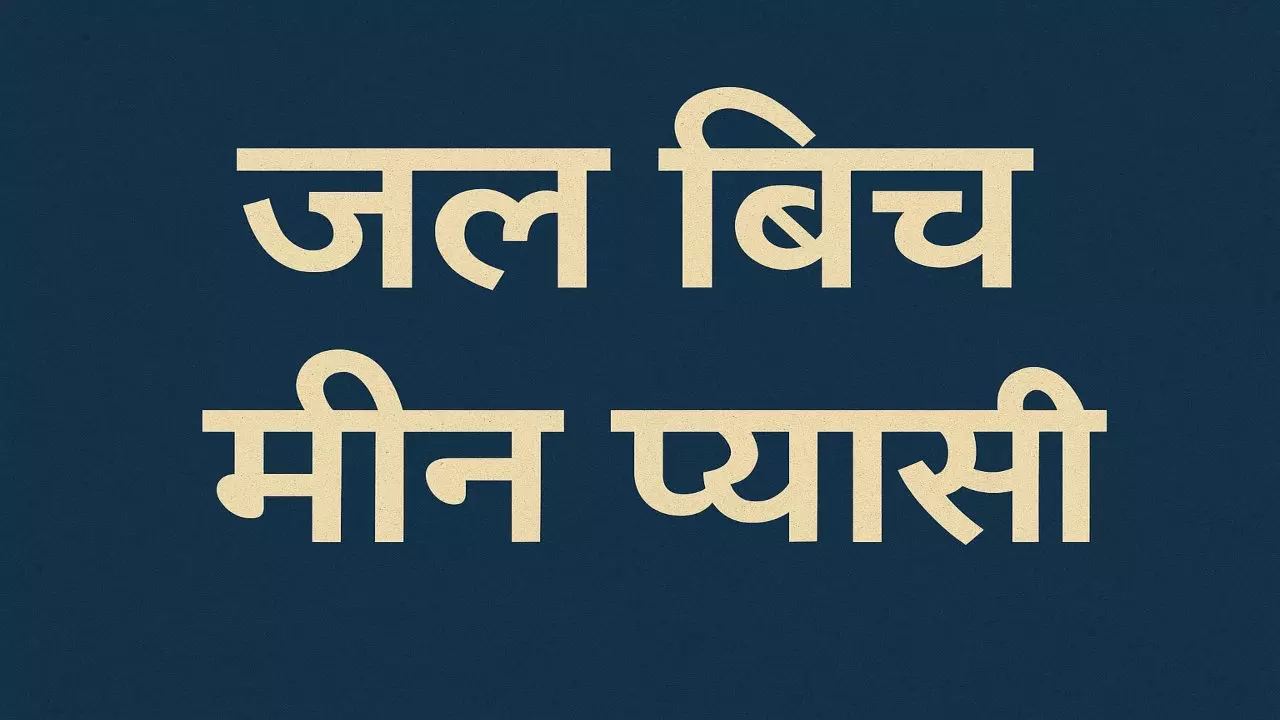TRENDING TAGS :
जल बिच मीन पियासी
Materialism and Modern Life: योगेश मिश्र का यह लेख भौतिकवाद की अंधी दौड़ और मनुष्य की अतृप्त प्यास पर गहरी चोट करता है।
Materialism and Modern Life (Image Credit-Social Media)
Materialism and Modern Life: यह लोकोक्ति महज़ एक रूपक नहीं है; इसका यथार्थ देखना हो तो वर्तमान में भौतिकवाद की दौड़ पर दृष्टि डाली जानी चाहिए। यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें उपलब्धियाँ क्षणभर में बौनी हो जाती हैं। मुट्ठी में आते ही भौतिकवाद की बड़ी से बड़ी चीज़ अपने एक नये विकल्प के साथ हमारे सामने खड़ी दिखाई पड़ती है। कुछ पा लेने की अर्थवत्ता भी बहुत कुछ खो देने की निरर्थकता के सामने एकदम बौनी होती जाती है। इस दौड़ में जाने-अनजाने हर कोई दौड़ रहा है। पता नहीं पराजय की निश्चितता के बाद भी यह दौड़ अनवरत क्यों जारी है? समझ में नहीं आता कि हम अभावों से घिरे व्यक्तियों के अभिशाप पर संवेदित हों या सुविधाओं से आकांत लोगों की महा-ऊब पर विलाप करें। क्या यह व्यर्थताबोध की सार्वभौमिक विजय का संकेत नित–नये पराजयों का फलक विकसित नहीं कर रहा है।
आज स्वयं को सुखी कौन कहता है? किसके पास संतोष का धन है? कौन संग्रह और त्याग के विवेक से सम्पन्न है? चारों ओर ‘चाहिए, और चाहिए, और चाहिए’ का विचित्र कोलाहल है। जो दूसरों का हिस्सा पचा चुके हैं, वे तीसरे और चौथे ‘हिस्से’ को पचाने का कार्यक्रम बना रहे हैं। इतना ही नहीं, अंशदारी के इस घोटाले को सामाजिक–राजनीतिक समस्या कहकर टालने की गम्भीर साज़िश भी चल रही है। यदि हम मनोविश्लेषकों पर विश्वास करें तो पाएँगे कि सदी भर पहले के मानव अधिक सहिष्णु, अधिक क्षमाशील—अर्थात अधिक मानवीय—थे। भौतिकवादी विकास एवं समृद्धि की अवधारणा के सामने मनोविश्लेषकों के इस निष्कर्ष को रखकर देखें तो साफ़ होता है कि विकास की इस अवधारणा में कोई गम्भीर खोट है—जिस खोट से आज समाज-निर्माण की ओर पहला कदम बढ़ाने वाले आदिपुरुष भी दुखी हैं, क्योंकि विकास के इस समीकरण में आदमी और मानवीयता हाशिये पर होते जा रहे हैं। विजय बहादुर सिंह के शब्दों में इसे ऐसे महसूस किया जा सकता है—
“मुझे ही बनाया गया था दुनिया का मालिक, निकाला गया मुझे ही सबसे पहले।
मेरे लिए ही रची गयी थी दुनिया, मुझे ही ख़ारिज किया गया सबसे पहले।”
मनोविश्लेषक यह भी कहते हैं कि जाति, वर्ग, भाषा, देश, रंग और सम्प्रदाय के सवालों को निरन्तर मनुष्य का रक्त पिलाया जा रहा है। कुछ शातिर व्यक्तियों की कोशिश है कि सहज रूप से जीने का सारा सुख समाप्त हो जाए—‘वे’ जैसे चाहें वैसे हम जीएँ। जब हम कहें कि हम तृप्त हैं—‘वे’ कहें कि नहीं, तुम अभी प्यासे हो। हमारी संतृप्ति के सवाल ‘वे’ ही तय करें। इन विकट बुद्धिजीवियों का शाश्वत प्रयोजन है कि मनुष्य पशु–स्तर पर—मशीनी स्तर पर—जीता रहे। तभी तो भौतिकवाद का इतना विस्तार किया जा रहा है कि आदमी हाशिये पर चला जाए, और जीवन की उच्च–उदात्त स्थितियों की ओर ताकना भी दुष्कर हो जाए। मनोविश्लेषकों ने एक स्वर से कहा है कि मशीनों का आदमी को ‘रिप्लेस’ करना ठीक नहीं—ऐसी मशीनों का ईजाद भी ठीक नहीं जो आदमी होने का दावा ठोंकती हैं—जैसे रोबोट। किसी समाज की मशीनों पर उतनी निर्भरता भी सुखद नहीं, जितनी आज दिखाई दे रही है। सच यह है कि आज पूरा समाज अबूझ किंतु दुर्दमनीय प्यास से छटपटा रहा है—जैसे जल के बीच रहने वाली मछली प्यास से उटपटाती रहती है।
यह बात दूसरी है कि हर व्यक्ति की प्यास की अपनी परिभाषाएँ हैं, अपने तर्क हैं, अपने परिप्रेक्ष्य हैं। मनुष्य गहराई में इस भ्रम में है कि उसे सुविधाएँ ही अंतिम रूप से संतृप्त कर सकती हैं। वह पता नहीं क्यों भूलता जा रहा है—“जब आवे सन्तोष धन, सब धन धूरि समान।” ‘ज़रूरत’ और ‘स्टेटस’ में अन्तर करने की हमारी कला निरन्तर क्षीण हो रही है। हमारे प्रदर्शक—अपने हित–चिन्तन के अनुसार—नागरिकों की कामनाएँ, आकांक्षाएँ उदीप्त कर रहे हैं। व्यक्ति ‘सेतु’ में होना चाहे तो उपभोक्तावादियों को आपत्ति है। व्यक्ति को सुराही श्रेष्ठ भले लगे, मगर महँगे फ़्रिज को ‘जीवन–मूल्य’ बना दिया गया है। व्यक्ति ने अपनी संज्ञा में जो विशेषण जोड़े हैं, वे गाड़ी, मोबाइल और मकान के आकार–प्रकार और स्तर के आगे फीके पड़ गये हैं। मेरे कई मित्र जो मुझसे मिलने घर या दफ़्तर आते हैं, वे प्रायः मेरी गाड़ी बाहर न खड़ी हो तो ‘मेरे नहीं होने’ का मन बनाकर वापस चले जाते हैं—उन्हें लगता है, मैं हूँ ही नहीं—गाड़ी मेरे होने का प्रमाण हो गई है। यदि किसी खास दोस्त को अपने उस मोबाइल नम्बर से फोन करता हूँ जो उनके फ़ोन में सेव नहीं, तो वे वह नम्बर नहीं उठाते—ऐसा मैं भी कर बैठता हूँ—शायद आप भी।
दौड़ आदमी–आदमी में नहीं है; व्यक्तित्व और कृतित्व के बीच भी नहीं; दौड़ केवल भौतिक वस्तुओं के बीच है—जो हमारी हैसियत में इज़ाफ़ा करती हैं और हमारी संज्ञा में विशेषण बनकर पैवस्त हो जाती हैं। आखिर ये जानलेवा प्रतियोगिताएँ, गला–काट स्पर्धाएँ क्या सिद्ध करना चाहती हैं? घूम–फिर कर चार्ल्स डार्विन के एक ही सिद्धांत का डंका बजाया जा रहा है—Survival of the fittest। विकासवाद के इस सिद्धांत को जिस सन्दर्भ में प्रयोग किया गया था, उससे काट दिया गया है। उसी ‘कटी हुई’ व्याख्या का परिणाम है कि नैतिकता, चारित्रिकता, मानवता, करुणा, दया, ममता, श्रद्धा, बलिदान, उत्सर्ग, उपकार और त्याग जैसे शब्द अपने असली अर्थ के लिए तरस रहे हैं। लम्बे समय से इनका उन सही सन्दर्भों में प्रयोग नहीं हुआ जिनके लिए वे बने थे। आज का समय ‘संक्रांति–काल’ तो है ही, ‘सम्भ्रांति–काल’ भी है—अनिश्चित मन, अनिश्चित भविष्य। मनुष्य किंकर्तव्यविमूढ़ है—उसे क्या पता कि वह जल में है और प्यास–प्यास चिल्लाती मीन की भाँति हास्यास्पद, दयनीय और चिंतनीय होता जा रहा है। ऐसी स्थितियों में निराला का कथन अपनी अर्थवत्ता में गम्भीर हो गया है—
“गहन यह अंधकार, स्वार्थ के अवगुंठनों से, हुआ है तुच्छ हमारा।”
प्रश्न है—क्या इस अंधकार से उद्धार सम्भव है? क्या आधुनिक सभ्यता के अमुचा (अनगढ़) व्यक्ति आम मनुष्य की छोटी–छोटी अभिलाषाओं का सम्मान सीख पाएँगे? क्या प्रकृति का दोहन लिप्सा के उपकरणों से यूँ ही होता रहेगा? समय उत्तर माँग रहा है। प्रकृति तो जननी है—उसके पास सच्ची प्यास का समाधान है—हमारी ही बुद्धि उससे युद्ध ठानती रहती है। इस युद्ध पर पुनर्विचार अपेक्षित है। कबीर ने वर्षों पूर्व इन्हीं सम्भावित स्थितियों को उलटबांसी में रख दिया था—महाकवि इसी अर्थ में काल का अतिक्रमण करते हैं; महापुरुष भी। वे इस द्वंद्व में किनारे खड़े होकर भौतिकवाद को ‘विजय’ की ओर जाते हुए चुपचाप देखते हैं, पर उसमें शामिल नहीं होते; उनका जीवन इतिहास के पन्नों में नया अध्याय दर्ज कराने को अहर्निश जुटा रहता है—क्योंकि वे ठीक से जानते हैं कि इस भौतिकवादी दौड़ में क्षण–क्षण, वस्तु–वस्तु पराजय निश्चित और निर्धारित है; इतने ढेर सारे लोग शामिल हैं कि उन्हें समझाकर मोड़ा नहीं जा सकता। कबीर ने यूँ ही नहीं कहा—
“पानी बिन मीन पियासी, मोहिं सुनि–सुनि आतप हाँसी।”
उपभोक्तावादी प्यास के मरुस्थल में चटकती मृगतृष्णाओं से उलझते मानव–समूह को इस हँसी से सावधान होना चाहिए। उसे एक दिन इन शब्दों में पुकारना ही होगा—
“मौला मुझे पानी दे, मैंने नहीं माँगा था
चाँदी की सुराही को, सोने के पिवाले को।”
आमीन।
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!