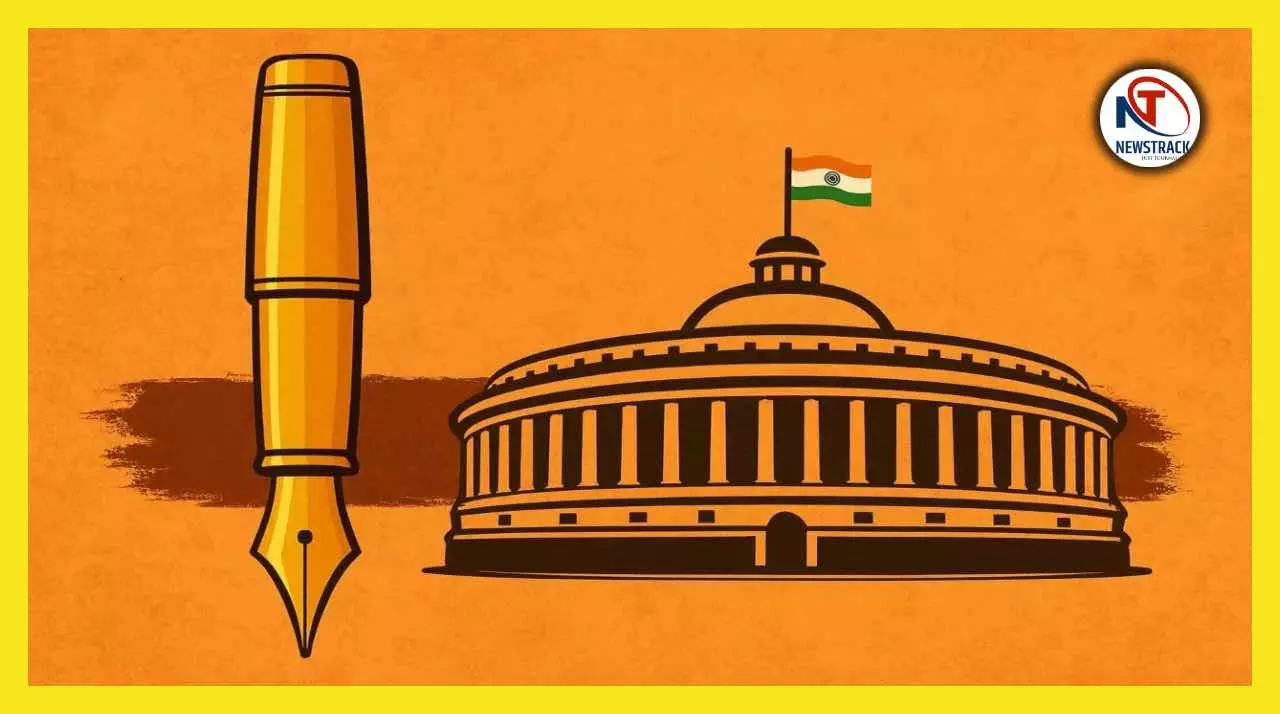TRENDING TAGS :
Akademi Award Return: पुरस्कार की राजनीति
Akademi Award Return: साहित्य अकादमी सहित कई पुरस्कारों की वापसी ने असहिष्णुता, राजनीति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गहन बहस छेड़ दी। योगेश मिश्रा का यह लेख पुरस्कारों की राजनीति और चुनिंदा विरोध के सवालों का विश्लेषण करता है।
Akademi Award Return
मुंशी प्रेमचंद ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि वह आने वाले किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनने का इंतजार कर रहे हैं। पर उन्होंने अपने समकालीन राजनीतिक दलों को साफ़ तौर पर महज़ इसलिए खारिज किया था ताकि वे यह बता और जता सकें कि राजनीति का साहित्य से और साहित्य का राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है। यह ज़रूर है कि साहित्य, राजनीति के आगे मशाल जलाती हुई चलने वाली एक सच्चाई है। लेकिन पिछले दो हफ्तों से जिस तरह हमारे साहित्यकार साहित्य अकादमी पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों की वापसी का क्रम चला रहे हैं, उससे तो लगता है कि हमारे साहित्यकारों ने मुंशी प्रेमचंद से कुछ नहीं सीखा।
जिस तरह के दावों और तर्कों का सहारा लेकर पुरस्कार वापस किए जा रहे हैं, उससे यह समझने में कोई संदेह नहीं रह जाता कि हमारे साहित्यकार बीती हुई पार्टी के हैं। बीते दो हफ्तों के इस वक्फ़े में पुरस्कार-वापसी के साथ इन्होंने जो भी तर्क दिए, अब साफ-साफ नज़र आने लगे हैं। अख़बारों से लेकर टी.वी. चैनलों तक और सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक—इनके विरोधियों द्वारा पूछे गए सवाल पुरस्कार-वापसी से ज़्यादा चर्चा में हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शायर मुनव्वर राणा तीन दिन में दो बार पलटी नहीं मारते। पहली बार वे पुरस्कार वापस करने वालों को नसीहत दे रहे थे, तो तीन दिन बाद मीडिया के ऑफिस में ही वे झोले में चेक और सम्मान-चिह्न लेकर आ धमके। क्या बेहतर नहीं होता कि वे बिना इन्हें लिए ही वापसी की घोषणा कर देते? क्या चेक और प्रतीक-चिह्न लेकर किसी चैनल के स्टूडियो में आना सियासत का हिस्सा नहीं है? उन्हें मैंने ख़ुद एक समय गन्ना संस्थान, लखनऊ में मायावती की तारीफ़ में कसीदे पढ़ते सुना। बाद में मुलायम के प्रति मुग्ध हुए। पुरस्कार वापस करने वालों में तमाम ऐसे नाम भी हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान खुले-आम मोदी का विरोध किया था—सरकार न बनने देने के लिए कोशिशें की थीं। सरकार बन गई तो भी उनका विरोध जारी रहा। लोकतंत्र में विरोध एक मज़बूत स्वर होता है, जो सत्ता पक्ष को नसीहत भी देता है, दिशा भी दिखाता है। लेकिन जब विरोध सिर्फ़ विरोध के लिए होने लगे तो उसके स्वर नक्कारखाने में तूती की आवाज़ बन जाते हैं।
पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकारों को बदलाव नरेन्द्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, एम.एम. कलबुर्गी और मोहम्मद अख़लाक़ की हत्या से उपजे माहौल से महसूस हो रहा है। इसी के चलते वे घुटन महसूस कर रहे हैं। देश में बढ़ रही कथित असहिष्णुता को लेकर हाय-तौबा कई सवाल खड़े कर रही है। इनका माकूल उत्तर मिले बिना पुरस्कार-वापसी का मन्तव्य किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम करने जैसा दिखने लगता है।
सवाल यह है कि आखिर जिस अख़लाक़ की मौत का रोना रोया जा रहा है, उसके लिए केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ज़िम्मेदार क्यों नहीं हो सकती? एम.एम. कलबुर्गी की हत्या कर्नाटक में हुई—वहाँ कांग्रेस की सरकार है। इसके लिए कांग्रेस को ज़िम्मेदार क्यों नहीं माना जाना चाहिए? नरेन्द्र दाभोलकर की हत्या जब हुई, तब केंद्र में डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार थी। आखिर उस समय साहित्यकारों को घुटन का अहसास क्यों नहीं हुआ?
इतिहास किसी का पीछा नहीं छोड़ता। भोपाल गैस कांड के समय साहित्यकार अशोक वाजपेयी का बयान किसी भी साहित्यिक संवेदना को तार-तार कर गया था। आज उन्हें घुटन का अहसास हो रहा है। मिलावट उजागर करने वाली वंदना शिवा को पुरस्कार मिलने के आस-पास ही मिलावट वाले शीतल पेय बेचने वाली कंपनी पेप्सी की इंद्रा नूयी को भी पद्म पुरस्कार देने पर क्यों नहीं हाय-तौबा मचाते हुए ये साहित्यकार दिखे?
डॉ. मनमोहन सिंह के अंतिम कार्यकाल में सुंदरता का बाज़ार तैयार करने वाली एक कंपनी के हवाले पद्म पुरस्कार कर दिया गया था। तब इन पुरस्कारों को लेकर गौरवान्वित होने वालों की आत्मा जाग्रत क्यों नहीं हुई? आपातकाल और 1984 के सिख विरोधी दंगों में भी भारतीय पारंपरिक सहिष्णुता मरती हुई इन्हें क्यों नहीं दिखी?
पुरस्कार वापस करने वाले साहित्यकार क्या सम्मानित होने के बाद मिली प्रतिष्ठा को भी वापस कर सकेंगे? पहले पुरस्कार पाने के लिए जतन करो, फिर वापसी की सियासत। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकसभा चुनाव के समय प्रख्यात कन्नड़ लेखक डॉ. यू.आर. अनंतमूर्ति ने यह बयान दिया था—“नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश रहने लायक नहीं रह जाएगा।” आखिर बड़े-बड़े पुरस्कार पाकर सम्मानित हुए बुद्धिजीवियों ने उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? वह भी तब, जब यह साफ़ था कि उनका दल बहुमत में होगा तभी वे प्रधानमंत्री बन सकेंगे। पुरस्कार की राजनीति और राजनीति के पुरस्कारों के चर्चे अब छिपे नहीं हैं। जिस साहित्य अकादमी के पुरस्कार लौटाए जा रहे हैं, वह एक स्वायत्त संस्था है। इन पुरस्कारों का फैसला लेखक मंडल करता है। उसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं—सिर्फ़ पुरस्कारों की राशि सरकार देती है। मतलब साफ़ है कि पुरस्कार लौटा कर आप सरकार को नहीं, ख़ुद को—अपनी बिरादरी को—कठघरे में खड़ा कर रहे हैं।
दरअसल, लेखकों की भूमिका में उनके इतिहास का योगदान न हो—ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना इतिहास के वर्तमान नहीं हो सकता—भविष्य तो बिल्कुल नहीं। अगर इतिहास पर नज़र डालें तो पुरस्कार-वापसी की अलख जगाने वाली नयनतारा सहगल, जवाहरलाल नेहरू की भांजी हैं। नयनतारा सहगल की तरह ही अशोक वाजपेयी भी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के ट्रस्टी रह चुके हैं। कोंकणी लेखक एन. शिवदास, गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। कन्नड़ लेखक हेमारेड्डी मालम्मा कथेय, अपनी एक किताब में एक स्थानीय संत के नाम पर ‘मर्डर मिस्ट्री’ लिखकर लोगों का विरोध झेल चुके हैं। गुरबचन सिंह भुल्लर अपनी प्रेस-रिलीज़ में यह तो कहते हैं कि पिछली सरकारों ने इस तरह की घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया—तो फिर करतूत सारी सरकारों की और विरोध-प्रदर्शन सिर्फ़ एक सरकार में? पुरस्कार लौटाने की अगली पांत में खड़ी सारा जोसेफ़ 2014 के लोकसभा चुनाव में केरल से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। ऐसी अनंत नज़ीरें हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि अगर एक उंगली पुरस्कार-वापसी की मार्फत नरेन्द्र मोदी की तरफ उठ रही है, तो चार उंगलियाँ अपनी तरफ भी हैं—इसका जवाब कौन देगा?
(मूलरूप से 27 अक्टूबर, 2015 को प्रकाशित। सितंबर, 2025 को संशोधित।)
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!