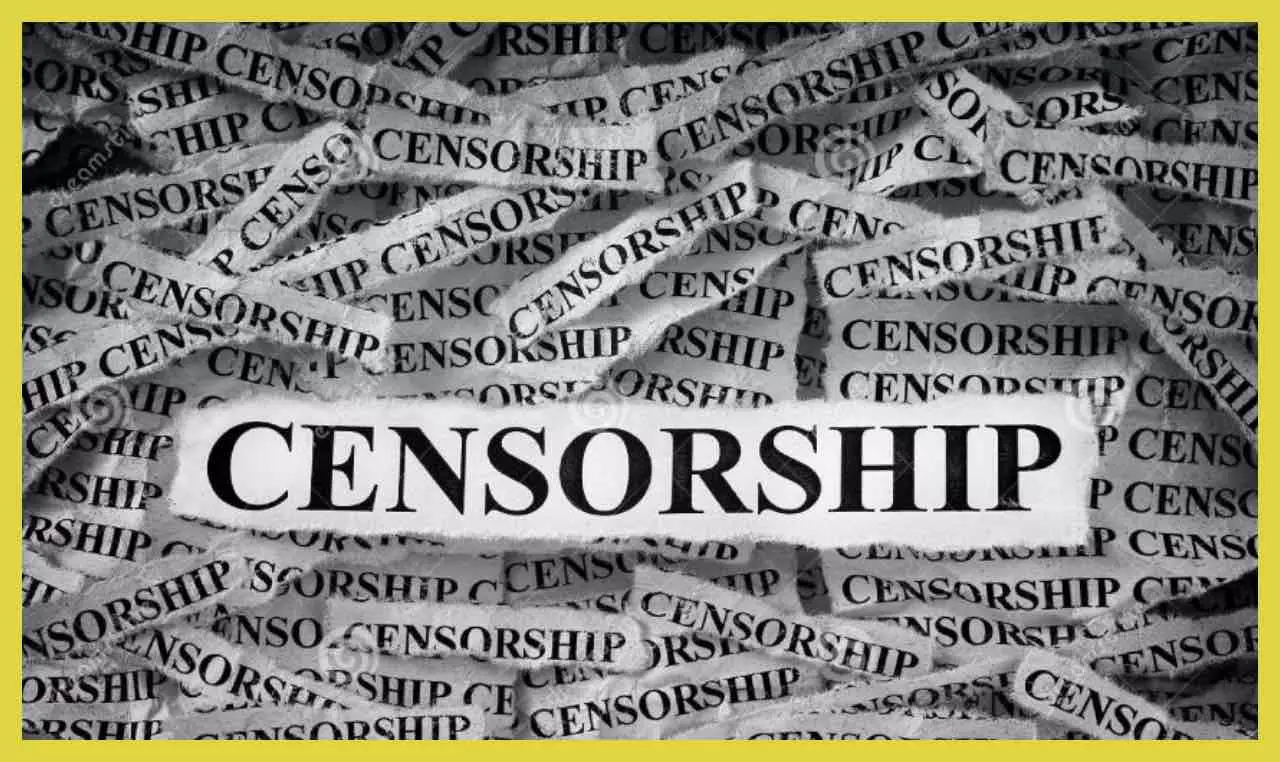TRENDING TAGS :
सेंसरशिप की प्रासंगिकता और विरोधाभास: एक वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य
Censorship Law in India: सेंसरशिप का मूल उद्देश्य यदि समाज को संरक्षित करना है, तो कई बार उसका दुरुपयोग भी हुआ है — विचारधारा, सत्ता और सामाजिक दबावों के चलते।
Censorship Law in India (Photo - Social Media)
Censorship Law in India: आज जब अभिव्यक्ति के लिए सोशल मीडिया, वेब सीरीज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म और स्वतंत्र फिल्म निर्माण का ज़माना है, वहीं "सेंसरशिप" (Censorship) शब्द भी एक नई बहस को जन्म देता है। यह नियंत्रण और स्वतंत्रता की रस्साकशी है, जिसमें कभी नैतिकता की जीत होती है और कभी विचारों की हत्या।
अमेरिका में सेंसरशिप: लोकतंत्र की सीमाएँ
संयुक्त राज्य अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान का पहला अधिकार (First Amendment) माना जाता है। फिर भी, हाल के वर्षों में कई उदाहरण देखने को मिले जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने किसी राजनैतिक विचार, धार्मिक मुद्दे या वैकल्पिक सोच को ‘सामुदायिक दिशानिर्देशों’ के नाम पर ब्लॉक कर दिया।
उदाहरणस्वरूप, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाना एक ऐतिहासिक और विवादास्पद फैसला था। कई विशेषज्ञों ने इसे ‘प्राइवेट सेंसरशिप’ कहा जो लोकतंत्र को प्रभावित कर सकता है।
भारत में सेंसरशिप: कला बनाम सत्ता
भारत में सेंसरशिप की भूमिका हमेशा बहस का विषय रही है, खासकर फिल्मों और वेब कंटेंट के संदर्भ में। सेंसर बोर्ड (CBFC) अक्सर नैतिकता और सार्वजनिक भावना के नाम पर फिल्मों में कटौती करता है — पर क्या ये हमेशा सही रहा है?
कुछ चर्चित सेंसरशिप केस:
उड़ता पंजाब (2016): पंजाब में ड्रग्स की समस्या पर बनी इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने 89 कट्स देने को कहा। शीर्षक से ‘पंजाब’ शब्द हटाने तक की सिफारिश की गई।
सवाल उठा – क्या हम सच्चाई से भाग रहे हैं
लिपस्टिक अंडर माय बुरखा (2017):
महिलाओं की यौन इच्छाओं और आत्म-अभिव्यक्ति पर बनी इस फिल्म को ‘बहुत बोल्ड’ बताकर रोक दिया गया। अंततः न्यायालय के हस्तक्षेप से यह रिलीज़ हो सकी।
पद्मावत (2018): ऐतिहासिक तथ्यों और कल्पना के मिश्रण को लेकर फिल्म का विरोध हुआ, करणी सेना ने इसे ‘राजपूत अस्मिता’ पर हमला बताया। सेंसर बोर्ड ने फिल्म का नाम बदला, कुछ दृश्य हटाए — मगर विवाद थमा नहीं।
तांडव (2021 - वेब सीरीज़): ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई इस सीरीज़ को लेकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। मेकर्स को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी और कई सीन हटाए गए।
सेंसरशिप: सुरक्षा या सेंसरशिप का दुरुपयोग
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि सेंसरशिप का मूल उद्देश्य यदि समाज को संरक्षित करना है, तो कई बार उसका दुरुपयोग भी हुआ है — विचारधारा, सत्ता और सामाजिक दबावों के चलते।
जरूरी सुधार:
फिल्म प्रमाणन बोर्ड में विविधता: सिर्फ नौकरशाही नहीं, बल्कि समाजशास्त्री, कलाकार और युवा प्रतिनिधि भी हों।
ट्रांसपेरेंसी: कौन से कट्स क्यों मांगे गए – इसका स्पष्ट ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए।
स्व-नियमन (Self-regulation): जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने किया है – निर्माता स्वयं जिम्मेदार बनें।
जनसंवाद: सेंसर के बजाय दर्शकों को परिपक्व मानते हुए विकल्पों का सम्मान किया जाए।
निष्कर्ष
सेंसरशिप आवश्यक है। लेकिन अंधी सेंसरशिप खतरनाक होती है। एक लोकतांत्रिक समाज में विचारों का संघर्ष स्वस्थ होता है, उसे कुचलना नहीं चाहिए। अगर किसी कंटेंट से समाज को खतरा है तो उसका समाधान संवाद और जागरूकता से हो — न कि कैंची से।
कला का काम सवाल उठाना है और सेंसरशिप तब तक स्वीकार्य है जब तक वह इन सवालों को दबाने का औज़ार न बन जाए।