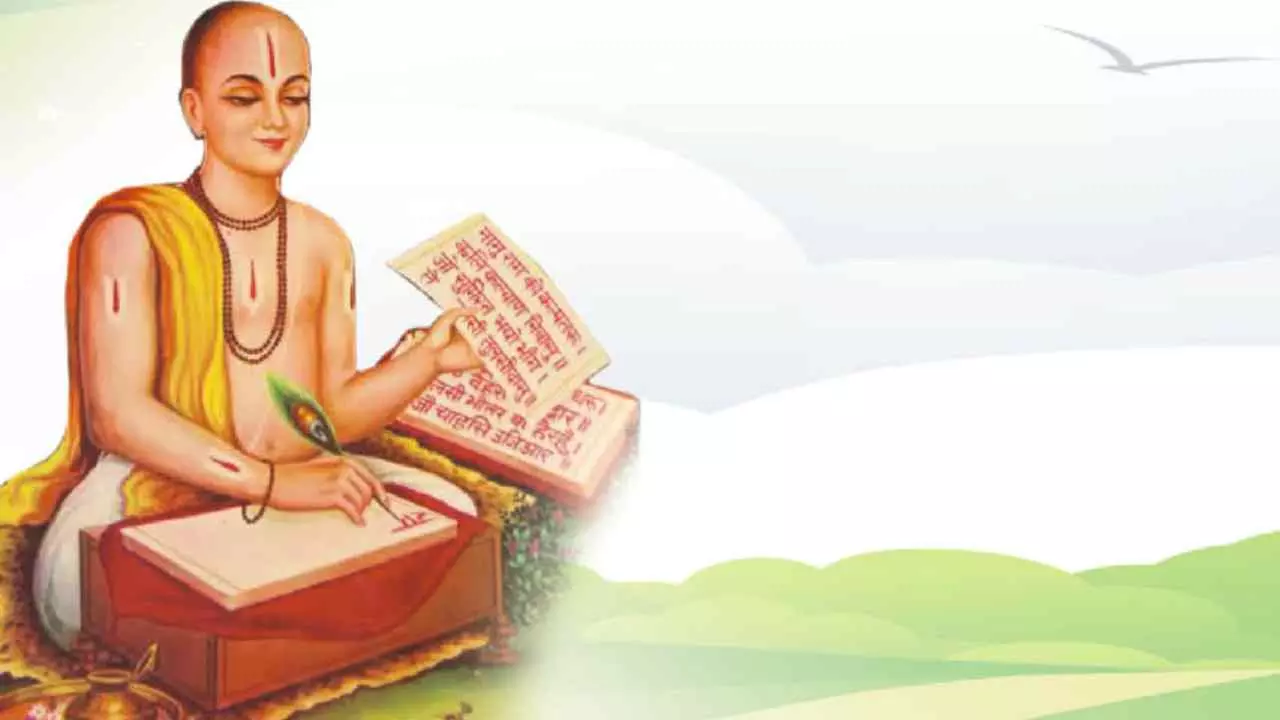TRENDING TAGS :
गोस्वामी तुलसीदास: भक्ति, भाषा और भारतीय चेतना के सार्वभौमिक स्तंभ
Goswami Tulsidas: तुलसीदास’( रामचंद्र शुक्ल): हिंदी साहित्य के महान आलोचक द्वारा लिखित प्रामाणिक एवं गहन अध्ययन। तुलसी के जीवन, काव्य और दर्शन का विश्लेषण।
Goswami Tulsidas (Image Credit-Social Media)
Goswami Tulsidas:
"राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरी द्वार।
तुलसी भीतर बाहेरहुँ जौं चाहसि उजिआर।।"
( हृदय रूपी द्वार की देहरी पर रूपमणि-सा राम नाम का दीपक रखो। तुलसीदास कहते हैं, अगर तुम भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश चाहते हो तो यही उपाय है।)
ये शब्द हैं भारतीय जनचेतना के सबसे प्रभावशाली एवं लोकप्रिय कवि-संत, गोस्वामी तुलसीदास के। उनकी कलम से निकली 'रामचरितमानस' ने न सिर्फ धार्मिक आस्था को नया आयाम दिया, बल्कि हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता को गढ़ने में अद्वितीय योगदान दिया। आज भी, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक, करोड़ों भारतीयों के दैनिक जीवन, आस्था और नैतिकता में उनकी उपस्थिति स्पष्ट झलकती है।
जन्म और प्रारंभिक जीवन: किंवदंतियों से घिरा एक संघर्षशील आरंभ
तुलसीदास का जन्म स्थान और समय ऐतिहासिक रूप से पूर्णतः स्थापित नहीं है, परन्तु प्रमुख मान्यताएँ इन्हें 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध (लगभग 1532 ई.) में राजापुर (वर्तमान चित्रकूट जिला, उत्तर प्रदेश) में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ मानती हैं। उनका बचपन का नाम रामबोला था। जन्म के समय ही उनके मुख में दांत होने और रोने की बजाय ‘राम’ बोलने की लोककथा प्रचलित है, जो उनकी दैवीय प्रतिभा की ओर इशारा करती है।
उनका बचपन विपत्तियों से भरा था। माना जाता है कि जन्म के कुछ समय बाद ही माता का देहांत हो गया और पिता ने भी उन्हें त्याग दिया। उनका पालन-पोषण एक दासी ने किया। कहते हैं पत्नी रत्नावली से अत्यधिक प्रेम के बावजूद उनके एक कटु वाक्य-
हाड़-मांस के देह मम तापर जौं प्रीति।
तौं ते सिय राम पै क्यों न होती।।
ने उनके जीवन को भक्ति की ओर मोड़ दिया और वे सांसारिक मोह को त्यागकर संन्यासी बन गए। उन्होंने श्रीराम के अनन्य भक्त संत श्री नरहरिदास से दीक्षा ली।
साहित्यिक यात्रा: अवधी को विश्वव्यापी पहचान दिलाने वाला महाकाव्य
तुलसीदास एक विपुल रचनाकार थे। उन्होंने दर्जन भर से अधिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें सबसे प्रमुख हैं:
1. रामचरितमानस (अवधी): यह तुलसीदास की अमर कृति है। इसे 'तुलसीकृत रामायण' या सिर्फ 'मानस' के नाम से भी जाना जाता है। सात कांडों (बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर) में विभक्त इस महाकाव्य ने संस्कृत के वाल्मीकि रामायण को अवधी भाषा के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाया। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन, नीति, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र और मानवीय मूल्यों का विश्वकोश है-
रघुपति राघव राजा राम,
पतित पावन सीताराम।
जैसे चौपाई और दोहे करोड़ों भक्तों की जिह्वा पर आज भी हैं।
2. विनय पत्रिका (ब्रज): राम के प्रति भक्ति, आत्मनिवेदन और विनय से भरपूर यह काव्य संग्रह तुलसी की गहन भक्ति भावना का प्रमाण है। कहा जाता है कि राम ने स्वयं इन पर हस्ताक्षर किए थे।
3. कवितावली (ब्रज): रामकथा का संक्षिप्त किंतु प्रभावी काव्यात्मक वर्णन।
4. गीतावली (ब्रज): रामकथा के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित गीतों का संग्रह।
5. दोहावली (ब्रज): नीति, भक्ति और समाजोपयोगी सूक्तियों का संग्रह।
6. हनुमान चालीसा (अवधी): हनुमानजी की स्तुति का अत्यंत लोकप्रिय छंद, जो करोड़ों हिंदुओं द्वारा नित्य पढ़ा जाता है-
बुद्धिहीन तनु जानिके,
सुमिरौं पवनकुमार..."
इसकी शुरुआती पंक्तियाँ हैं।
7. पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न: अन्य महत्वपूर्ण रचनाएँ।
गहन धार्मिक प्रभाव: भक्ति के सागर में अवगाहन
तुलसीदास का धार्मिक प्रभाव अतुलनीय और व्यापक है:
रामभक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ: वे रामानंद के परंपरा के प्रमुख संत थे। उन्होंने 'राम' को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित किया, जो सर्वसामान्य के लिए आराध्य, अनुकरणीय और प्रेम करने योग्य हैं।
सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा: उन्होंने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण (रूप, गुण और लीला वाले) राम की उपासना को जन-जन तक पहुँचाया। उनका राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी मानवीय करुणा, प्रेम और कर्तव्यपरायणता से ओतप्रोत हैं।
मर्यादा का संदेश: 'रामचरितमानस' का मूल आधार 'मर्यादा' (नैतिकता, अनुशासन, कर्तव्यपालन) है। पिता का आदेश पालन (वनवास), पत्नी का सम्मान (सीता का त्याग नहीं), भाई का प्रेम (भरत-राम प्रेम), प्रजा के प्रति कर्तव्य - ये सब मर्यादा के उदाहरण हैं जो जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं।
भक्ति की सरलता: तुलसी ने भक्ति को जटिल कर्मकांडों और जातिगत बंधनों से मुक्त किया। उन्होंने घोषित किया-
जाति-पाँति पूछे नहिं कोई।
हरि को भजै सो हरि का होई।।
और-
संत समाज वेद विधि जे निंदहिं।
तिन्ह कर कुकिरित सुनि रामु सिंधहिं।।"
उनकी भक्ति सहज, सरल और हृदय से निकलने वाली थी।
सामाजिक समरसता: उन्होंने नारी जाति (सीता, अनुसुइया, अहिल्या का गौरव), शूद्रों (निषादराज, केवट) और वनवासियों (शबरी) को भक्ति में उच्च स्थान दिया, जो तत्कालीन समाज में क्रांतिकारी था। हनुमानजी जैसे वानर सेवक को उन्होंने भक्ति का आदर्श बनाया।
धार्मिक एकता का बीज: 'मानस' ने सम्पूर्ण भारत में रामकथा को एक सूत्र में बांधा, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त विविध धार्मिक प्रथाओं के बीच एकता का सूत्रपात हुआ।
तुलसीदास पर प्रमाणित स्रोतों से लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें:
1. ‘तुलसीदास’( रामचंद्र शुक्ल): हिंदी साहित्य के महान आलोचक द्वारा लिखित प्रामाणिक एवं गहन अध्ययन। तुलसी के जीवन, काव्य और दर्शन का विश्लेषण।
2. ‘गोस्वामी तुलसीदास’ ( धीरेन्द्र वर्मा): जीवनी और साहित्यिक विवेचन का संतुलित ग्रंथ।
3. ‘तुलसीदास और उनका युग’ ( विश्वनाथ प्रसाद मिश्र): तुलसीदास के जीवनकाल के ऐतिहासिक-सामाजिक संदर्भ को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
4. ‘तुलसी साहित्य में लोकमंगल’ ( रामकुमार वर्मा): तुलसी के साहित्य में निहित जनकल्याणकारी भावना पर केन्द्रित।
5. ‘ तुलसीदास की भक्ति भावना’ ( मैनेजर पाण्डेय): तुलसी की भक्ति दर्शन की विस्तृत व्याख्या।
6. "Tulsidas: Poet, Saint and Philosopher" (F.R. Allchin): अंग्रेजी में एक प्रसिद्ध अध्ययन।
7. "Tulsidas: L'Homme et l'Oeuvre" (Françoise Mallison - फ्रांस्वा ग्रॉसार्ड): फ्रेंच विद्वान द्वारा गहन शोधपूर्ण कार्य (फ्रेंच में)।
प्रासंगिकता: आज क्यों जीवित हैं तुलसीदास?
नैतिक मूल्यों का आधार: 'मानस' आज भी भारतीय समाज के लिए नैतिकता, कर्तव्य, परिवारिक मूल्य, सत्य और अहिंसा का सबसे बड़ा स्रोत है। राम-रावण का संघर्ष आज भी अच्छाई-बुराई के संघर्ष का प्रतीक है।
भाषाई एकता का प्रतीक: 'मानस' की अवधी भाषा उत्तर भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत है। इसके दोहे और चौपाइयाँ घर-घर में समझे जाते हैं, भाषाई विविधता के बावजूद।
सामाजिक समरसता का संदेश: जाति, लिंग या वर्ग के भेद से ऊपर उठकर मानवता और भक्ति पर उनका जोर आज के विभाजित समाज में अत्यंत प्रासंगिक है। शबरी और निषादराज का उदाहरण समावेशिता सिखाता है।
आध्यात्मिक सुख का मार्ग: भौतिकवाद के इस युग में, उनका संदेश - राम नाम के सुमिरन से मिलने वाली आंतरिक शांति और सुख - मानसिक तनाव से मुक्ति का मार्ग दिखाता है।
सांस्कृतिक पहचान: रामलीलाओं, भजनों, प्रवचनों और दैनिक पाठ के माध्यम से 'मानस' भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग बना हुआ है।
तुलसीदास का स्वप्न: रामराज्य की अवधारणा
तुलसीदास ने 'रामराज्य' की जो अवधारणा 'मानस' (उत्तरकांड) में प्रस्तुत की, वह उनके आदर्श समाज का दर्पण है:
नैतिक शासन: जहाँ राजा प्रजा के लिए त्याग करने को तत्पर रहे, न्यायप्रिय हो और धर्म के मार्ग पर चले-
“दैहिक दैविक भौतिक तापा।
राम राज नहिं काहुहि ब्यापा।।"
( शारीरिक, दैविक और भौतिक कष्ट किसी को भी नहीं सताते।)
सुखी एवं धार्मिक प्रजा: जहाँ प्रजा धर्मपरायण, सदाचारी, परिश्रमी और सुखी हो। चोरी, झूठ, अनाचार का भय न हो-
“नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना।
नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना।।"
प्रकृति एवं मनुष्य का सामंजस्य: जहाँ पशु-पक्षी भी निर्भय होकर विचरण करें।
आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक शांति: जहाँ अकाल न पड़े, समृद्धि हो और सामाजिक कलह न हो।
भक्ति का केन्द्रीय स्थान: जहाँ राम का नाम सर्वत्र गूंजता हो।
कालजयी प्रेरणा के स्रोत
गोस्वामी तुलसीदास कोई साधारण कवि नहीं थे; वे एक सांस्कृतिक क्रांति के सूत्रधार थे। उन्होंने जटिल दार्शनिक सत्यों को सरल, सरस और हृदयस्पर्शी काव्य के माध्यम से जनसाधारण तक पहुँचाया। उनकी 'रामचरितमानस' ने भारतीय समाज को एक सूत्र में बाँधा, हिंदी भाषा को अमरत्व प्रदान किया और सनातन धर्म को एक नया, सर्वग्राह्य रूप दिया। उनका संदेश - प्रेम, भक्ति, नैतिकता, कर्तव्यपालन और सामाजिक समरसता का - आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना चार शताब्दी पूर्व था। जब तक भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा अस्तित्व में रहेगी, तुलसीदास का नाम अमर रहेगा। वे सच्चे अर्थों में भारतीय आत्मा के अनवरत प्रवाह को दिशा देने वाले सदा बहने वाले स्रोत हैं।
स्रोत एवं तथ्य-जांच: इस लेख में प्रस्तुत जानकारी उपरोक्त उल्लिखित प्रमाणित पुस्तकों (रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि), प्रतिष्ठित विद्वानों के शोधपत्रों, 'रामचरितमानस' एवं तुलसीदास के अन्य मूल ग्रंथों के अध्ययन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा अन्य शोध संस्थानों के अभिलेखागारों में उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री, और तुलसीदास से जुड़े प्रामाणिक स्थलों (राजापुर, अस्सी घाट, चित्रकूट) के ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है। किंवदंतियों को उनके ऐतिहासिक-सांस्कृतिक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!