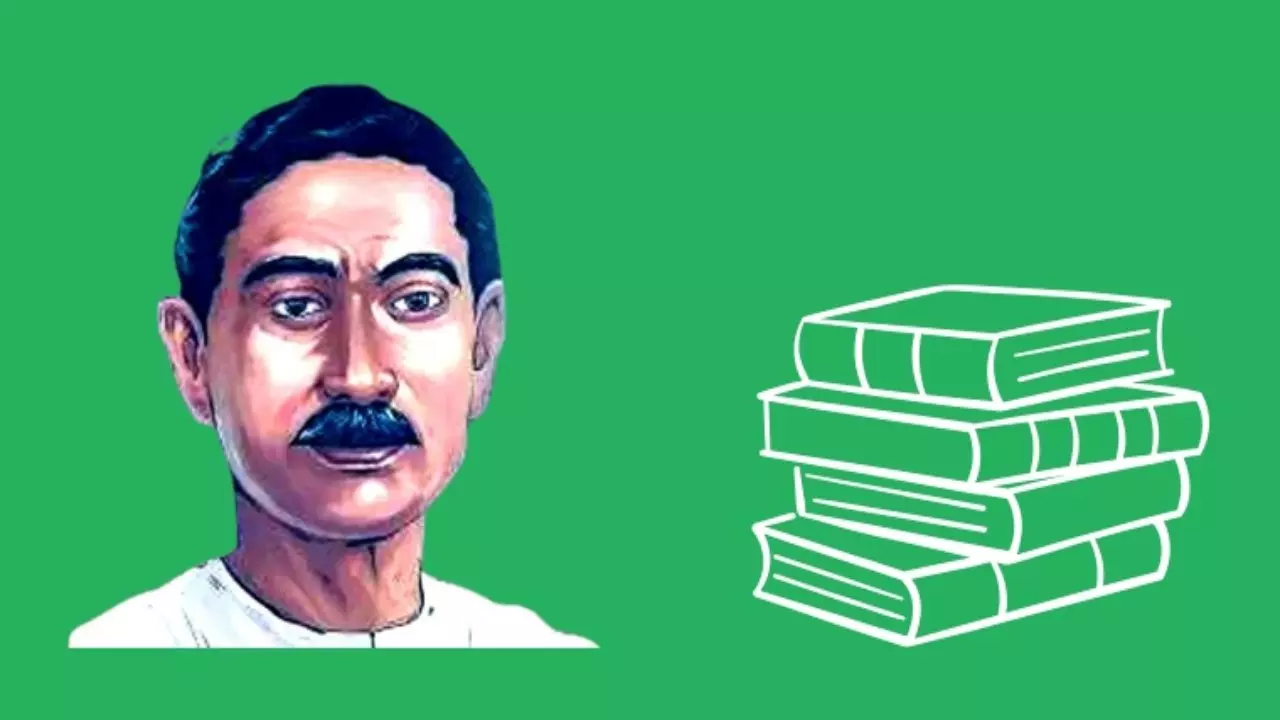TRENDING TAGS :
प्रेमचंद और संविधान: वो सामाजिक सपने जो कहानियों से सदन तक पहुँचे
Premchand : प्रेमचंद की रचनाओं में सामाजिक न्याय समानता और मानवाधिकारों के सिद्धांत को बेहद ख़ूबसूरती से दर्शाया गया है। आइये जानते हैं क्या है इनकी खासियत।
Premchand (Image Credit-Social Media)
प्रश्न: क्या प्रेमचंद की कहानियों में ऐसे तत्व मौजूद थे, जो बाद में भारत के संविधान में भी झलके?
उत्तर: हाँ, प्रेमचंद की रचनाओं में सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के जो सिद्धांत बार-बार उभरे, वही सिद्धांत भारतीय संविधान (1950) की आधारशिला बने। यह समान सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक साझा विचारधारा का प्रतिबिंब था, न कि प्रेमचंद से सीधे उधार लिया गया। दोनों ने अपने-अपने समय की जटिल सामाजिक व्यवस्था की चुनौतियों का जवाब दिया।
मुख्य तथ्यों का विश्लेषण एवं प्रमाणिक स्रोत
1. जातिगत भेदभाव एवं अस्पृश्यता का विरोध (समानता - अनुच्छेद 14-18):
प्रेमचंद: "सद्गति" (दुखी की मौत), "ठाकुर का कुआँ", "कफन" जैसी कहानियाँ जातिगत ऊँच-नीच, अमानवीय भेदभाव और शोषण की मार्मिक तस्वीर पेश करती हैं। "सद्गति" का दुखी इस व्यवस्था की क्रूरता का प्रतीक बन गया।
संविधान: अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), अनुच्छेद 15 (धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध), अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत), अनुच्छेद 18 (उपाधियों का अंत)।
सम्बन्ध व तथ्य: प्रेमचंद ने जिस क्रूर यथार्थ का चित्रण किया, संविधान ने उसे गैर-कानूनी घोषित किया। प्रेमचंद का वर्णन सामाजिक न्याय की मांग को दर्शाता है, जो संविधान का मूल लक्ष्य बना।
स्रोत: प्रेमचंद की मूल कहानियाँ ("मानसरोवर" संग्रह), भारतीय संविधान का मूल पाठ (अनुच्छेद 14-18)।
2. सामाजिक न्याय एवं पिछड़े वर्गों का उत्थान (अनुच्छेद 15(4), 16(4), 46):
प्रेमचंद: "गोदान" का होरी (गरीब किसान), "कफन" के घीसू-माधव (वंचित तबका) - प्रेमचंद ने समाज के निचले पायदान पर जीवन की पीड़ा और उनके उत्थान की जरूरत को गहरी संवेदनशीलता से उकेरा। उनकी कृतियाँ शोषण के खिलाफ आवाज़ थीं।
संविधान: अनुच्छेद 15(4) और 16(4) (SC/ST और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण/विशेष प्रावधान), अनुच्छेद 46 (SC/ST और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा)। प्रस्तावना में "सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय" का लक्ष्य।
सम्बन्ध व तथ्य: प्रेमचंद ने जिन वंचितों के दुख को चित्रित किया, संविधान ने उन्हें न्याय और उन्नति का संवैधानिक अधिकार दिया। प्रेमचंद ने समस्या को पहचाना, संविधान ने समाधान का मार्ग प्रशस्त किया।
स्रोत: उपन्यास "गोदान", कहानी "कफन", भारतीय संविधान (अनुच्छेद 15(4), 16(4), 46, प्रस्तावना)।
3. स्त्री अधिकार एवं समानता (अनुच्छेद 14, 15, 21):
प्रेमचंद: "निर्मला" (बाल विवाह, वृद्ध पति के साथ विवाह का दुष्परिणाम), "सेवासदन" (वेश्या जीवन में धकेली गई स्त्री, समाज का दोहरा मापदंड), "बड़े घर की बेटी" (स्त्री शिक्षा और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता) जैसी रचनाओं में उन्होंने महिलाओं के प्रति होने वाले अन्याय, दहेज प्रथा, बाल विवाह और उनकी शिक्षा व स्वतंत्रता की मांग को सशक्त ढंग से उठाया। निर्मला का चरित्र स्त्री-शोषण का प्रतीक है।
संविधान: अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 15 (लिंग के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार - जिसे बाद में गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार तक विस्तृत माना गया)। स्त्री शिक्षा और विकास पर जोर।
सम्बन्ध व तथ्य: प्रेमचंद ने स्त्री जीवन की त्रासदियों को केंद्र में रखकर समाज को झकझोरा। संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान का कानूनी आधार दिया। प्रेमचंद ने स्त्री-पीड़ा को साहित्य का विषय बनाया, संविधान ने उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा।
स्रोत: उपन्यास "निर्मला", "सेवासदन", भारतीय संविधान (अनुच्छेद 14, 15, 21)।
4. गरीब किसान व मजदूरों का शोषण (अनुच्छेद 23, 24, 39, 43):
प्रेमचंद: "गोदान" का होरी साहूकारों और जमींदारों की शोषण प्रणाली का शिकार है। "पूस की रात" किसान की विवशता और प्रकृति के प्रकोप को दर्शाती है। उनकी रचनाओं में किसानों और मजदूरों की दुर्दशा और उनके शोषण के विरुद्ध आक्रोश स्पष्ट है।
संविधान: अनुच्छेद 23 (मानव दुर्व्यापार एवं बलात श्रम का प्रतिषेध), अनुच्छेद 24 (बाल श्रम पर प्रतिबंध), अनुच्छेद 39(क) (जीविकोपार्जन के साधनों का समान वितरण), अनुच्छेद 43 (कामगारों को निर्वाह योग्य मजदूरी, काम की उचित शर्तें)। राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) कल्याणकारी राज्य की अवधारणा देते हैं।
सम्बन्ध व तथ्य: प्रेमचंद ने ग्रामीण शोषण की क्रूरता को उजागर किया। संविधान ने श्रमिकों के शोषण को रोकने और उनके कल्याण के लिए ठोस प्रावधान किए। प्रेमचंद ने आर्थिक अन्याय का यथार्थ चित्रण किया, संविधान ने उसे दूर करने के राज्य के कर्तव्य निर्धारित किए।
स्रोत: उपन्यास "गोदान", कहानी "पूस की रात", भारतीय संविधान (अनुच्छेद 23, 24, भाग IV - राज्य के नीति निदेशक तत्व विशेषकर 39, 43)।
5. धर्मनिरपेक्षता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव (अनुच्छेद 25-28, प्रस्तावना):
प्रेमचंद: "मंदिर और मस्जिद", "ईदगाह" जैसी कहानियाँ हिंदू-मुस्लिम एकता और मानवीय रिश्तों को धर्म से ऊपर रखती हैं। उनका साहित्य सांप्रदायिकता की निंदा और साझा मानवीय मूल्यों पर जोर देता है।
संविधान: अनुच्छेद 25-28 (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार), प्रस्तावना में "पंथनिरपेक्ष" (Secular) शब्द (1976 में जोड़ा गया, लेकिन मूल ढांचा धर्मनिरपेक्ष था)। सभी नागरिकों को बिना धार्मिक भेदभाव के समान अधिकार।
सम्बन्ध व तथ्य: प्रेमचंद ने साम्प्रदायिक सद्भाव और मानवता को सर्वोपरि रखा। संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता के साथ-साथ राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को स्थापित किया। **प्रेमचंद ने सांप्रदायिक विषबीज के खतरे को पहचाना, संविधान ने उसके निवारण का संस्थागत ढांचा दिया।
स्रोत: कहानियाँ "मंदिर और मस्जिद", "ईदगाह", भारतीय संविधान (अनुच्छेद 25-28, प्रस्तावना)।
साहित्यिक पूर्वाभास और संवैधानिक अभिव्यक्ति
सीधा प्रभाव नहीं, साझा दृष्टि: यह दावा करना गलत होगा कि संविधान निर्माता सीधे तौर पर प्रेमचंद की कहानियों से प्रेरित थे। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि प्रेमचंद और संविधान निर्माता (डॉ. अंबेडकर, पं. नेहरू सहित) एक ही ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ (जातिगत उत्पीड़न, स्त्री-अधिकारों की अनदेखी, गरीबी, सांप्रदायिकता) से जूझ रहे थे और उसी प्रबुद्ध भारतीय चेतना (जाति-धर्म से ऊपर उठकर मानवीय गरिमा, समानता, न्याय) से प्रभावित थे।
साहित्य: समाज का दर्पण और प्रेरक: प्रेमचंद का यथार्थवादी साहित्य उस समय के भारत की क्रूर सामाजिक-आर्थिक विषमताओं का शक्तिशाली दस्तावेज है। इसने समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति जागरूकता फैलाई और परिवर्तन की मांग को मजबूत किया। यह सामूहिक चेतना का निर्माण करने में सहायक हुआ।
संविधान: कानूनी ढांचा और सपनों का आधार: संविधान ने उन्हीं सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने और एक न्यायपूर्ण, समतामूलक समाज बनाने के लिए कानूनी ढांचा और मौलिक सिद्धांत प्रदान किए। यह प्रेमचंद जैसे लेखकों द्वारा उजागर की गई समस्याओं का संस्थागत समाधान और भविष्य का खाका था।
अंतिम बात: प्रेमचंद की कहानियाँ और भारतीय संविधान, दोनों ही भारत के सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के संघर्ष और सपने की दो अलग-अलग किंतु परस्पर पूरक अभिव्यक्तियाँ हैं। प्रेमचंद ने जमीनी हकीकत को कलमबद्ध कर समाज को झकझोरा, तो संविधान ने उस हकीकत को बदलने के लिए कानूनी हथियार दिए। यह साहित्य की वह शक्ति है जो सपनों को कानून का रूप लेने की प्रेरणा दे सकती है।
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!