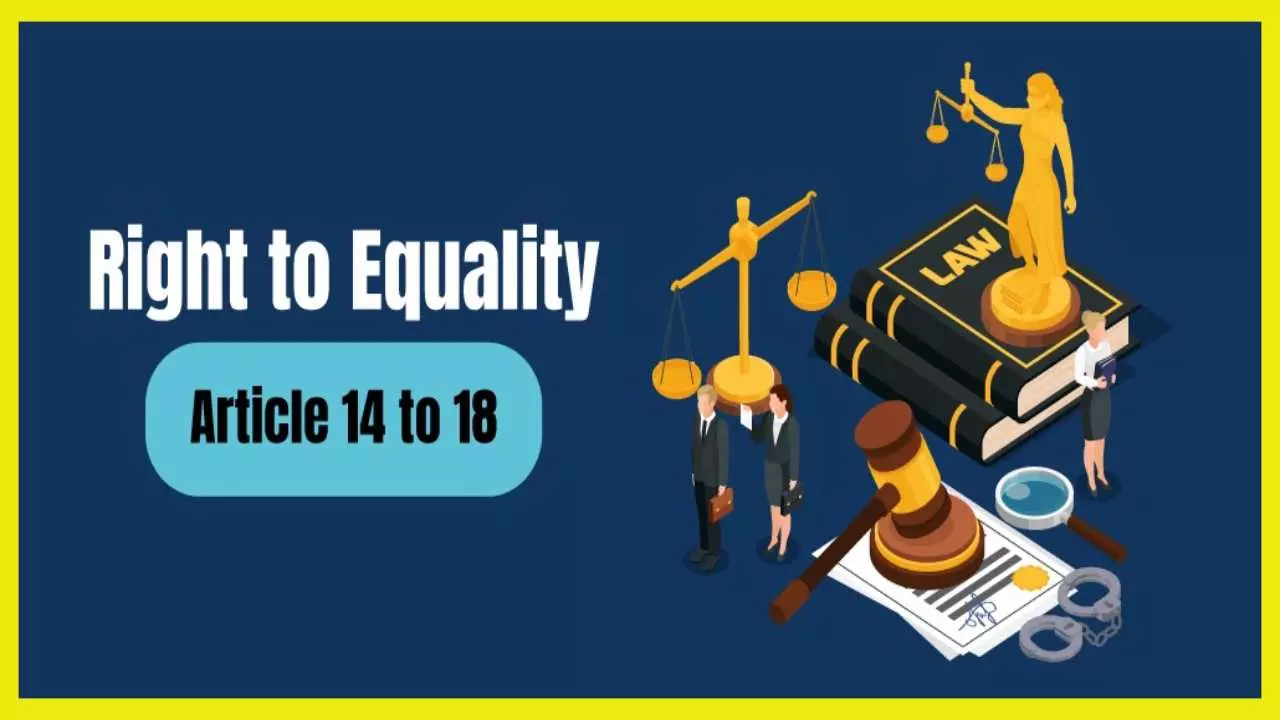TRENDING TAGS :
भारत में समानता का अधिकार: संवैधानिक आदर्श और कठोर यथार्थ
Right to equality in India: अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता से जुड़े विस्तृत प्रावधान हैं। लेकिन क्या कागजों पर लिखे ये आदर्श देश की विविध और जटिल सामाजिक संरचना में पूरी तरह उतर पाए हैं?
Right to equality in India (Image Credit-Social Media)
Samanta Ka Adhikar: भारत का संविधान ‘समानता के अधिकार’ को मौलिक अधिकारों में स्थान देकर एक समतामूलक समाज की नींव रखता है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता से जुड़े विस्तृत प्रावधान हैं। लेकिन क्या कागजों पर लिखे ये आदर्श देश की विविध और जटिल सामाजिक संरचना में पूरी तरह उतर पाए हैं? आइए, तथ्यों और आंकड़ों की कसौटी पर जांचें।
संवैधानिक बुनियाद: मजबूत ढांचा
अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण।
अनुच्छेद 15: धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध। सरकार को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (विशेषकर एससी/एसटी) के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार।
अनुच्छेद 16: लोक नियोजन में अवसर की समानता। आरक्षण का प्रावधान।
अनुच्छेद 17: ‘अस्पृश्यता’ का उन्मूलन (कानूनन अपराध)।
अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत (सैन्य/शैक्षणिक को छोड़कर)।
ये प्रावधान दुनिया के सबसे प्रगतिशील संविधानों में शुमार हैं।
यथार्थ की जमीन: चुनौतियां और प्रगति
1. लैंगिक असमानता: लंबी जद्दोजहद
श्रम भागीदारी: विश्व बैंक (2023) के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर लगभग 37% है, जो वैश्विक औसत (47%) और कई विकासशील देशों से काफी नीचे है। (स्रोत: विश्व बैंक डेटाबेस)
मजदूरी अंतर: वेतन में लैंगिक अंतर बना हुआ है। मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स (2023) के अनुसार, भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाएं औसतन 28% कम कमाती हैं।
शिक्षा में प्रगति, पर सशक्तिकरण अधूरा: साक्षरता दर (2011 जनगणना) में महिलाओं की 65.46% बनाम पुरुषों की 82.14%। हालांकि, शिक्षा में नामांकन दरों में काफी सुधार हुआ है। फिर भी, रोजगार और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी सीमित।
हिंसा और सुरक्षा: एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) 2022 के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,45,256 मामले दर्ज हुए। दहेज हत्या (14,247), बलात्कार (31,878) और घरेलू हिंसा के मामले चिंताजनक हैं।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व: संसद में महिला सांसदों का प्रतिशत लगभग 15% (2024) है, जो वैश्विक औसत (26.5%) से काफी कम है। (स्रोत: इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन)
2. जातिगत असमानता: गहरी पैठी विषमता
सामाजिक भेदभाव: अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के खिलाफ भेदभाव और अत्याचार के मामले आज भी सामने आते हैं। एनसीआरबी 2022 के अनुसार, एससी के खिलाफ 57,582 और एसटी के खिलाफ 11,451 मामले दर्ज हुए। इसमें अत्याचार निवारण अधिनियम (पीओए) के तहत दर्ज मामले शामिल हैं।
आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन: सामाजिक-आर्थिक जनगणना (2011) और विभिन्न रिपोर्ट्स दर्शाती हैं कि एससी/एसटी समुदायों की आय, भूमि स्वामित्व और उच्च शिक्षा तक पहुंच औसत से काफी नीचे है।
आरक्षण का प्रभाव: शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण ने इन समुदायों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, इसकी प्रभावकारिता और भविष्य को लेकर सामाजिक-राजनीतिक बहस जारी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10% आरक्षण एक नया प्रयास है।
3. धार्मिक अल्पसंख्यक: चिंताएं बरकरार
मुस्लिम समुदाय: सच्चर समिति रिपोर्ट (2006) और पीवीएसआरएफ (पीपुल्स रिपोर्ट ऑन इकोनॉमिक सिचुएशन, 2023) जैसी रिपोर्टें लगातार दर्शाती हैं कि मुस्लिम समुदाय शिक्षा, रोजगार और आर्थिक संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से पीछे है।
सामाजिक एकता और भेदभाव: हाल के वर्षों में धार्मिक रेखाओं पर सामाजिक तनाव और अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव के आरोपों और घटनाओं (जैसे लिंचिंग, घर वापसी जैसे अभियान) ने समानता के अधिकार पर सवाल खड़े किए हैं। (स्रोत: विभिन्न स्वतंत्र मानवाधिकार रिपोर्ट्स, जैसे एपीआरएफ, ह्यूमन राइट्स वॉच)
4. एलजीबीटीक्यू+ समुदाय: शुरुआती कदम, लंबा सफर
ऐतिहासिक फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में धारा 377 को आंशिक रूप से रद्द कर समान लिंग के वयस्कों के बीच सहमति से संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। यह एक बड़ी जीत थी।
वर्तमान चुनौतियां: समान-लिंग विवाह को कानूनी मान्यता नहीं है। सामाजिक कलंक, भेदभाव, हिंसा और स्वास्थ्य व रोजगार जैसे बुनियादी अधिकारों तक पहुंच में बाधाएं गंभीर समस्या हैं। परिवार और सामाजिक स्वीकृति एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
5. आर्थिक असमानता: बढ़ती खाई
ऑक्सफैम इंडिया की "सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट" रिपोर्ट (2023) के अनुसार, भारत में शीर्ष 10% के पास देश की कुल संपत्ति का 77% हिस्सा है, जबकि निचले 60% के पास महज 4.8% संपत्ति है। कोविड-19 ने इस असमानता को और बढ़ाया है।
सकारात्मक पहल और प्रयास
कानूनी ढांचा: अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम (पॉश), ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम जैसे कानून मौजूद हैं।
सरकारी योजनाएं: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्टैंड-अप इंडिया, शिक्षा और स्वास्थ्य में विशिष्ट योजनाएं, एससी/एसटी के लिए विशेष घटक योजनाएं।
न्यायपालिका: सुप्रीम कोर्ट ने समानता के अधिकार को व्यापक रूप से परिभाषित करते हुए कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं (धारा 377 का निरसन, सबरीमाला मामले में महिलाओं के प्रवेश का अधिकार, विवाहित महिलाओं के पिता की संपत्ति में अधिकार आदि)।
सामाजिक जागरूकता: नागरिक समाज, मीडिया और शिक्षा के माध्यम से समानता के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
आदर्श और यथार्थ के बीच का फासला
भारत में समानता का अधिकार एक जटिल और बहुआयामी तस्वीर पेश करता है। संविधान ने एक मजबूत और प्रगतिशील आधार तो दिया है, और कुछ क्षेत्रों (जैसे शिक्षा तक पहुंच, कानूनी सुधार) में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हालांकि, गहराई से जड़ जमाए सामाजिक पूर्वाग्रह, आर्थिक विषमता, जाति और लिंग आधारित भेदभाव, और धार्मिक अल्पसंख्यकों व यौनिक अल्पसंख्यकों के प्रति व्यवस्थित चुनौतियां अभी भी बड़ी बाधाएं हैं।
संवैधानिक समानता को वास्तविक जीवन में अनुभव होने वाली समानता में बदलने के लिए केवल कानून काफी नहीं है। इसके लिए सतत सामाजिक सुधार, शिक्षा के माध्यम से मानसिकता में बदलाव, कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, आर्थिक अवसरों का न्यायसंगत विस्तार और हर स्तर पर भेदभाव के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की आवश्यकता है। भारत की समानता की यात्रा अधूरी है, लेकिन संविधान द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शक सिद्धांत और नागरिकों की बढ़ती जागरूकता इस दिशा में आशा की किरण बनी हुई है। सही मायनों में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' तभी साकार हो पाएगा जब समानता का अधिकार हर नागरिक की जिंदगी की हकीकत बनेगा।
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!