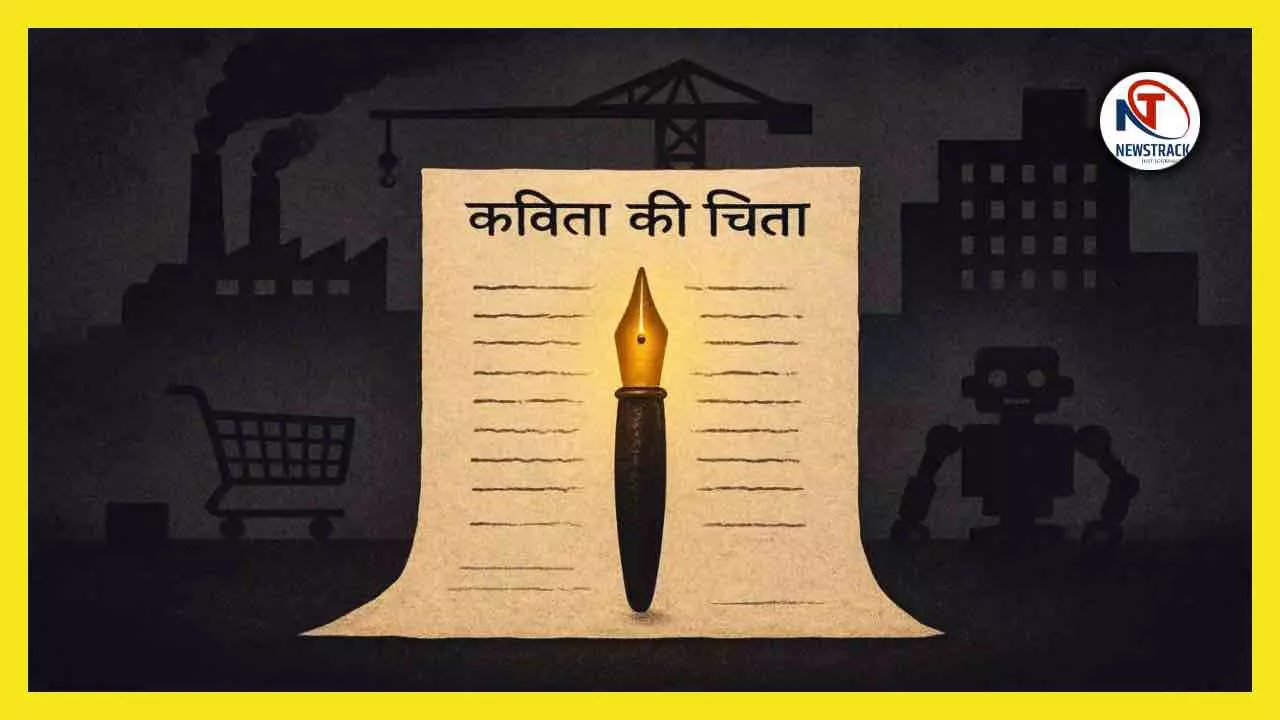TRENDING TAGS :
Hindi Poetry: कविता की चिन्ता
Hindi Poetry: योगेश मिश्र का यह लेख कविता की संवेदनशीलता, जनसरोकार और समकालीन काव्य पर बाज़ारवाद के प्रभाव की गहरी पड़ताल करता है।
Hindi Poetry: लोकोन्मुख प्रतिबद्धता के अभाव में साहित्य की कोई भी विधा महान नहीं हो सकती—कविता, नई कविता, अकविता, आधुनिक कविता के संदर्भ में यह धारणा आज आम होती जा रही है। भाववादी कविता बुद्धिवादी हो गई है; भाव उसमें से विलोपित हो गया है; भाव से पहले गेयता विलुप्त हो चुकी है। कविता की नयी यात्रा में कई मज़ाक कविता के हमक़दम हो गए हैं। कवियों की संख्या में इज़ाफ़ा जारी है, लेकिन काव्य का संवेदना से रिश्ता टूटता जा रहा है। काव्य जनोन्मुखी नहीं रह गया; लोकहित का वाहक नहीं बन पा रहा। कविता का सम्बन्ध हृदय से नहीं, मस्तिष्क से जुड़ रहा है। नूतन अलंकरणों और अपने कर्म का औचित्य सिद्ध कर सकने की तर्क–शक्ति से संपन्न आज के अनेक कवि ऐसी कविताएँ लिख रहे हैं जो संगठित राजनीति—खासकर संगठित राज्य–शक्ति—की क्रूरताओं को शांत, चिकनी, आत्मलिप्त चासनी की भाषा में परोस रही हैं; वे ऐसी अदा में अपनी बात कहते हैं कि अपने वर्ग के मूलभूत आचरण में निहित दोगलेपन पर कोई चोट न लगे—“साँप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे” सरीखी भूमिका बनती जा रही है।
कविता की इन स्थितियों से—राज्य–शक्ति की क्रूर भावनाओं के खिलाफ खड़े होने की ताकत के अभाव में—पाठक कविता से कटने लगा। उसे लगा कि लेखक अपने दायित्व के निर्वाह से वंचित हो रहा है। बाज़ार–तंत्र का ऐसा कुप्रभाव हुआ कि कविगण अपनी कविता में सुलभ संवेदनशीलता और वैचारिक प्रगतिशीलता के बावजूद अत्यंत आत्मवद्ध स्थितियों के माध्यम से ही जीवन–वस्तु थोड़ी बहुत मात्रा में ला पाते हैं।
जबकि एक समय में कविता समूचे समाज की जटिलता और संश्लिष्टता को एक खास कोण से ‘फोकस’ करने का काम करती थी—उसके साधारण शब्द भी असाधारण आकार रखते थे। कविता सिर्फ अर्थ–ग्रहण तक ही नहीं थी, उससे बिंब–ग्रहण भी अपेक्षित था—वह नदी, तालाब, पेड़–पौधे, फूल, बाग–बगीचे में भी जीवन्त बिंब डाल देती थी। अंतरविरोधों से जूझने का अवसर हो या विरोधाभासों से लड़ने का मौका, इतिहास–बोध की स्थापना की ज़रूरत आन पड़ी हो—सही समय पर जीवन–संसार के विराट सत्व से साक्षात्कार करने, भीतर–बाहर के संसार से लड़ने—इन सब में कविता ने अनेक विधाओं और कलाओं से बड़ी भूमिका निभाई है; वह हृदय का बंधन खोलती है।
बाज़ारवाद और उससे प्रेरित आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक प्रभाव ने आज के काव्य–संसार को काफ़ी प्रभावित किया है। कविता के कथ्य और शिल्प पर गौर किया जाए तो साफ़ दिखता है कि शिल्प के विविध प्रयोगों के विस्तार की धरातल पर कहीं कथ्य धुंधलाया है और कहीं मनुष्य की चेतनागामी आवाज़ कुछ कमजोर हुई है—हालाँकि कविता मनुष्य को लोक–सामान्य भाव–भूमि पर ले जाती है; वह मनोविकारों का परिष्कार करती है; चर–अचर के साथ रागात्मक सम्बन्ध बनाती और निभाती है।
यही कारण है कि कविता अपने यथार्थ से कटती हुई दिखने लगी है। कविता की यथार्थवादी प्रकृति के लिए कवि की विचारात्मक प्रतिबद्धता जितनी ज़रूरी नहीं, उससे अधिक ज़रूरी है समाज की बहुआयामी विविधताओं से उसका परिचय। जबकि स्थिति यह है कि समाज की मध्यवर्गीय स्थितियों एवं नगरीय आपाधापी ने कवि को श्रमिक और जनता के दैनिक जीवन से विलगा दिया है। कवि के पास अपने चित्रण के लिए प्रत्यक्ष–साक्षात्कार का समय नहीं रहा; वह कविता को संगणक की तर्ज़ पर देखने–स्वीकारने लगा है; गरीबी, भूख, यातना के चित्रण के लिए उसे कल्पना का सहारा लेना पड़ता है—यह कहना कि “मृत्यु के चित्रण के लिए मरना आवश्यक नहीं” आत्म–घटित से साक्षात्कार से काट लेने वाला कुतर्क है—क्योंकि संचार–सूचना साम्राज्य के दौर में गरीबी–भूख–यातना और ऐसे हृदयविदारक दृश्य बार–बार देखकर हम प्रभावहीन हो चले हैं; पहले देह की प्रतिक्रिया निस्संग हुई—अब आत्मा भी कई सवालों पर चुप्पी ओढ़ लेती है।
इसीलिए आत्म–अनुभूत को आत्म–अनुभूति के स्तर पर जीने की जो विशेषता कवियों–साहित्यकारों में हुआ करती थी, वह क्षीण हुई। विषय–वस्तु के अभाव से शिल्प के अभ्यास पर से कवि का नियंत्रण ढीला पड़ा; परिणामतः प्रगतिशील वैचारिक रुझान के बावजूद परोक्ष रूप से पूंजीवादी–विज्ञापनवादी राज्य–सत्ता का औचित्य–स्थापन करती कविता दिखाई पड़ने लगी। इस तरह कविता और जनता के बीच भाषा–अभिव्यक्ति की एक चौड़ी खाई खिंच गई, जिसमें भाषा अर्थ से विच्छिन्न हो जाती है। पिछली सदी में मलार्मे ने कहा था—कविता केवल शब्दों में रची जाती है; वे भूल गए कि शब्दों के उत्स भाव और महत्त्व भी होते हैं। भाषा महज़ शब्द–प्रयोग नहीं है—यदि ऐसा होता तो ‘सार्थक’ और ‘निरर्थक’ शब्द–भेद क्यों होते? कविता भाषा का सघन प्रयोग है—इसीलिए तुलसीदास जन–मानस के चिरंजीवी कवि बनते हैं और केशव एक समुदाय–विशेष तक सीमित। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा था—केशव को ‘कृषि–हृदय’ नहीं मिला—क्योंकि उनके यहाँ मलार्मे–प्रेरित ‘शब्द–प्रधानता’ का आग्रह था। निष्कर्ष साफ़ है—भाव–योग के स्थगित होते ही रचना–योग भी ठहरने लगता है। भाव–शक्ति से ही कोई काव्य कालजयी बनता है; भाव हमारे साहित्य का बुनियादी तत्व है—मनुष्य में भाव की चिर–भूख है—कविता का काम उसी भूख को शांत करना है—और राज्य–सत्ता के दोगलेपन पर आक्रमण करना भी।
इसीलिए कविता के भाव–बोध से कटने के बाद भी उसके यथार्थवाद को सहज स्वीकार किया गया था; पर आज कविता इस दायित्व से भी विमुख दिख रही है। कवि दलीय चेतनाओं, राज्य–सत्ता से संरक्षण–लाभ की आशाओं के कारण स्पष्ट कह पाने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। अपवादस्वरूप कुछ विरले कवियों के रचनात्मक दायित्वों को छोड़ दें तो समकालीन काव्य–परिदृश्य में अधिकांश कवियों के सरोकार और चिंताएँ निजी, वर्गीय और वैयक्तिक होती जा रही हैं—यह चिंता का विषय है।
कविता की चिंता में सम्प्रेषण भी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। कविता पर आरोप है कि जनता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा; वह स्मृतियों में नहीं ठहर रही। परम्परा से ही जनता की दृष्टि में कवि का सम्मान रहा है—तो आज वह क्यों घटा? समकालीन कविता अपने स्वरूप–चरित्र में एक–सी नहीं—वह एक समय में लिखी जा रही अनेक प्रकार की कविताओं का समूह है—इसलिए उसके बारे में कोई भी निष्कर्ष समग्र पर लागू नहीं होता। दस अच्छी कविताओं के साथ दस कमजोर कविताएँ भी मिलेंगी। भाषा के मामले में कुछ ऐसी रचनाएँ भी होंगी जिनकी भाषा आम सम्प्रेषण की नहीं—अत्यन्त कलात्मक—सघन प्रतीकों की बारीक कलात्मकता—जो आस्वाद और सम्प्रेषण के स्तर पर कुछ विशेष कलावंतों/पाठकों का विषय हो सकती हैं, पर व्यापक जन–समुदाय का नहीं। समकालीन कविता दार्शनिक भी है और जटिल भी—यही कारण है कि कविता की किताब ख़रीदकर या पुस्तकालयों से निकालकर आज के कवि की कविता सामान्य पाठक नहीं पढ़ रहा।
आम लोगों में फ़्रांसीसी कवि एटियेन (स्तेफ़ान) मलार्मे का कथन पैठ गया, पर हमें—हमारे साहित्य को—कालजयी होने के लिए जन–वाद में भटकाव–मूलक रुझानों से कटकर या तो यथार्थवाद स्वीकारना होगा या कविता को हृदय से जोड़ना होगा—क्योंकि यही दृष्टि कविता की रचनात्मक समस्याओं को समझने–सुलझाने की एकमात्र सही दृष्टि है; वही कवि और समाज के मध्य परस्पर–प्रभावकारी सम्बन्ध के यथार्थ को व्याख्यायित कर सकती है। इसके सिवा जो कुछ भी है—वह कविता के हित में नहीं—क्योंकि समकालीन कविता में अभिव्यक्ति और समाज–बोध का जो संकट है, वह उसी वाद–खेमेबाज़ी की देन है जिसमें कविता लगातार उलझी जा रही है—जबकि लिखते समय कोई भी कवि पूरी तरह ‘वाद–मुक्त’ होता है; उसकी समूची कविता उसके आत्म–घटित/आत्म–अनुभूति की सघन वेदनात्मक परिणति होती है। तभी तो कहा गया—“वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान; निकलकर नयनों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान।”
यदि हम अपनी पक्षधरता–प्रतिबद्धता से ही मुक्त होकर साहित्य–कर्म में रत रहेंगे तो कविता–साहित्य के कालजयी होने के लिए कुछ करने की गुंजाइश शेष नहीं बचेगी—क्योंकि हमारी प्रतिबद्धताएँ समयगामी और अवसरगामी हैं; उसी का नतीजा है कि ‘दलित–साहित्य’ को केवल वही स्वीकार्य मानने का आग्रह उभरा है जिसे दलितों ने ही रचा—और दावा किया जाने लगा कि गैर–दलित ‘दलित–साहित्य’ रच ही नहीं सकता।
मूल रूप से कविता का एक प्रयोजन ‘शिवेत्तर क्षय’—अर्थात अमंगल तथा जन–विरोधी प्रवृत्तियों का विनाश—है। इस दृष्टि से कविता की आलोचना मनुष्यता की समग्र परिधि में ही संभव है—यह बात अलग है कि उसकी मौलिकता समय के साथ रूपान्तरित होती रहती है। इस कसौटी पर आज हमारे पास बहुत कम ऐसी कविताएँ हैं जिनमें समय को समग्रता से पढ़ा और महसूस किया जा सके। किसी आलोचक ने ठीक ही कहा—“जब कवि का स्टेथोस्कोप मनुष्य की छाती पर न रखकर कैलेंडर के पन्नों पर रखा जाएगा तो दिक़्क़तें पैदा होंगी।” हमें महाकवि निराला की पुकार “जागो फिर एक बार” के अर्थ को सामयिक परिवेश में जाग्रत करना होगा। यह भी स्मरण रहे—शब्द कभी मरते नहीं। समग्र लोकधर्मी परम्परा किसी भी प्रकार की वादीयता से कमजोर पड़ती है—कविता में वादी–चेतना का बंधन नहीं, मनुष्य–दृष्टि का विस्तार होना चाहिए—इसी दिशा में की गई काव्य–सर्जना सार्थक होगी। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने चिन्तामणि में लिखा—“ज्यों–ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नये–नये आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों–त्यों एक ओर कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी”—पर दूसरी ओर कविकर्म भ्रमित भी होता जाएगा। इस विरोधाभास से बचने का समय है—क्योंकि यदि ऐसा न हुआ तो मनुष्य एवं संवेदना के बीच के रिश्तों की मातम–पुर्ती करनी पड़ेगी।
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!