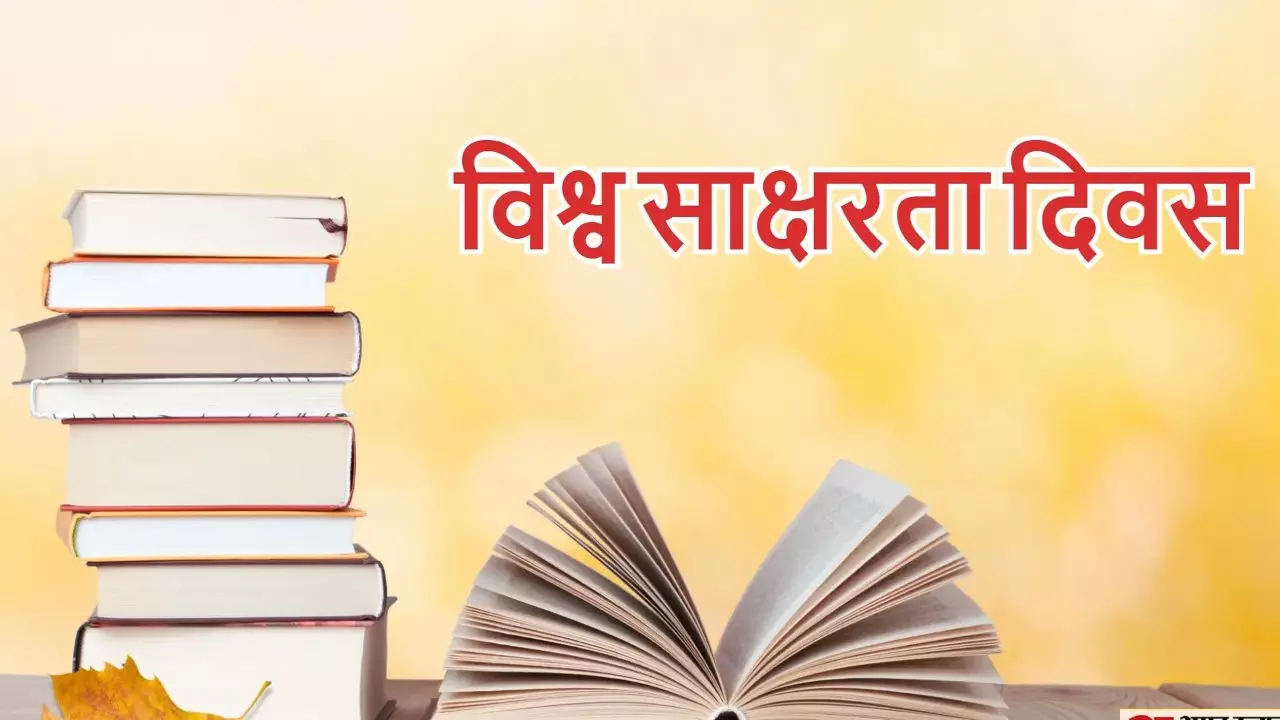TRENDING TAGS :
अक्षर से अवसर तक- क्यों जरूरी है विश्व साक्षरता दिवस का संदेश
World Literacy Day 2025: विश्व साक्षरता दिवस की आधारशिला यूनेस्को द्वारा तय की गई थी। जिसका उद्देश्य था निरक्षरता को मिटाना और शिक्षा की लौ हर घर तक पहुंचाना।
World Literacy Day 2025 (Image Credit-Social Media)
World Literacy Day: आदि काल से अब तक इंसान ने जिस तरह धरती से अंतरिक्ष तक की दूरी तय की है इसके पीछे अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की है, तो वह है ज्ञान। ज्ञान बिना साक्षरता के संभव नहीं। मनुष्य के जीवन में धन से कहीं ज्यादा अकूत संपत्ति ज्ञान को माना जाता है। यही ज्ञान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी दुनिया में करोड़ों लोग आज भी इस ज्योति से वंचित हैं। अक्षर न पहचान पाने की यह कमी केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अवसरों से भी वंचित कर देती है। साथ ही सामाजिक विकास की तरक्की में भी बाधा बनती है। इसी पीड़ा को समझते हुए दुनिया हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व और सामाजिक विकास, देश की तरक्की के प्रति अपना नैतिक कर्तव्य भी है। आइए जानते हैं विश्व साक्षरता दिवस से जुड़े इतिहास और विभिन्न पहलुओं के बारे में -
कैसे रखी गई विश्व साक्षरता दिवस की आधारशिला
विश्व साक्षरता दिवस की आधारशिला यूनेस्को द्वारा तय की गई थी। पूरी दुनिया में लोगों को साक्षर करने का बीड़ा उठाते हुए सन 1965 में यूनेस्को ने यह तय किया कि 8 सितंबर को शिक्षा और साक्षरता के नाम समर्पित किया जाएगा। अगले ही वर्ष 1966 में पहली बार यह दिवस मनाया गया। जिसका उद्देश्य था निरक्षरता को मिटाना और शिक्षा की लौ हर घर तक पहुंचाना। इसके बाद 2003 से 2012 तक पूरे दशक को संयुक्त राष्ट्र ने 'साक्षरता दशक' घोषित किया। यूनेस्को द्वारा की गई यह पहल केवल औपचारिक प्रयास तक सीमित नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया में अभियान के तहत लोगों एक जुट कर साक्षरता के महत्व को समझाने का एक गंभीर प्रयास था। ताकि दुनिया के हर कोने तक इंसान के व्यक्तिव का विकास हो सके।
क्या है वैश्विक साक्षरता की स्थिति
तकनीक और आधुनिकता की इस दुनिया में भी साक्षरता का स्तर चिंता पैदा करता है। यूनेस्को के अनुसार वर्ष 2024 तक करीब 76 करोड़ लोग अब भी साक्षर नहीं हैं। इनमे दो-तिहाई महिलाएं हैं, जिनकी शिक्षा तक पहुंच बहुत सीमित रही है। एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में निरक्षरता सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं विकसित देशों में भी समस्या अलग है। वहां पढ़ना-लिखना तो आता है, लेकिन उसका व्यवहारिक उपयोग नहीं हो पाता। इससे साफ है कि शिक्षा का असली मतलब केवल अक्षरों को पहचानना नहीं, बल्कि उन्हें जीवन में उतारना है।
भारत में साक्षरता की स्थिति
भारत की साक्षरता यात्रा भी उतार-चढ़ाव से भरी रही है। 1951 की जनगणना में साक्षरता दर मात्र 18 प्रतिशत थी। 2011 तक यह 74 प्रतिशत तक पहुंच गई और आज अनुमान है कि यह 80 प्रतिशत के करीब है। लेकिन आंकड़े पूरी सच्चाई नहीं बताते। केरल जैसे राज्य लगभग शत-प्रतिशत साक्षर हैं, तो वहीं बिहार अब भी सबसे नीचे है। गांवों में शिक्षा की सुविधाओं की कमी, गरीबी, बाल श्रम और लड़कियों की शिक्षा को लेकर सामाजिक सोच अब भी बड़ी रुकावट हैं।
व्यावहारिक ज्ञान के साथ साक्षरता क्यों जरूरी है?
साक्षरता जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यह रोज़गार के बेहतर अवसर देती है, समाज में समानता लाती है और इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है। शिक्षित माता-पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य को बेहतर दिशा दे पाते हैं। लोकतंत्र की नींव भी तभी मजबूत होती है जब उसके नागरिक शिक्षित और जागरूक हों। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि यह इंसान को जीने का सही तरीका सिखाती है।
साक्षरता दिवस बन चुका है अब एक वैश्विक उत्सव
हर साल इस दिन पर देश-दुनिया में सेमिनार, रैलियां और जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। कहीं बच्चों को किताबें बांटी जाती हैं, तो कहीं गरीब बस्तियों में जाकर शिक्षा का महत्व समझाया जाता है। परंतु सच यह है कि केवल कार्यक्रमों से बदलाव नहीं आता। असली बदलाव तब होता है जब हम खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाते हैं। साक्षरता का यह यज्ञ तभी सफल होगा जब हम उसमें अपनी छोटी-सी आहुति देंगे।
छोटे कदम, बड़ा असर और हमारी भूमिका
अगर हमारे भीतर खुद को साक्षर करने के साथ ही साथ अपने आसपास समाज में भी बदलाव करने की चाहत है तो इस ओर हमारा छोटे से छोटा प्रयास भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। संभव है कि हमारी पहुंच हर उस बच्चे तक संभव न हो पाएं, लेकिन किसी एक भी गरीब बच्चे को स्कूल भेजने में मदद करके ही हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी के साथ ही मोहल्ले में छोटे-छोटे अध्ययन समूह बनाकर बच्चों को पढ़ाना भी एक पहल हो सकती है। मजदूर परिवारों से बात करके उन्हें यह समझाया जा सकता है कि शिक्षा उनके बच्चों का भविष्य बदल सकती है। उनके साथ सरकार की लाभकारी योजनाओं और छात्रवृत्तियों की जानकारी साझा करना भी उनके जीवन में साक्षरता के प्रति नई रोशनी जगा सकता है। यानी हमारे द्वारा किए गए छोटे-छोटे प्रयास किसी के जीवन की दिशा बदल देते हैं।
साक्षरता बढ़ाने के प्रयास और सरकारी योजनाओं की पहल
भारत सरकार भी साक्षरता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। मिड-डे मील योजना बच्चों को पौष्टिक भोजन देकर स्कूल में बनाए रखती है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी योजनाएं लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। वयस्कों के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 भी महत्वपूर्ण कदम हैं।
शिक्षा सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी
अक्सर लोग शिक्षा को केवल रोजगार पाने का साधन मान लेते हैं, लेकिन इसके प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। शिक्षा सोचने की क्षमता देती है, आत्मसम्मान जगाती है और इंसान को चुनौतियों से लड़ने की ताकत देती है। यह हमें बेहतर इंसान बनाती है और समाज को बेहतर दिशा देती है। इसलिए शिक्षा को केवल पैसे या नौकरी तक सीमित देखना इसके महत्व को कम करना है।
भारत में शिक्षा के प्रचार की पहल
भारत में शिक्षा का प्रचार-प्रसार बहुत लम्बा और विविधतापूर्ण सफर रहा है। अलग-अलग कालखंडों में कई महापुरुषों, समाज सुधारकों और संस्थाओं ने शिक्षा को आम जनता तक पहुंचाने की पहल की। इस दिशा में प्रमुख नाम और उनकी भूमिका इस प्रकार है:
प्राचीन और मध्यकाल के दौरान
तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में ही उच्च शिक्षा का वैश्विक केंद्र रहे। भक्ति और सूफी संत कबीर, नानक, संत तुकाराम, रहीम आदि ने सरल भाषा में शिक्षा और ज्ञान का प्रचार किया ताकि आमजन तक इसकी पहुंच कायम हो सके।
आधुनिक काल (ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता आंदोलन)
ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में राजा राममोहन राय स्त्रियों की शिक्षा और आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रबल समर्थक। उन्होंने हिन्दू कॉलेज (कोलकाता, 1817) की स्थापना में योगदान दिया।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि बालिका शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के समर्थक। उन्होंने बंगाल में कई कन्या पाठशालाएं शुरू कराईं।
ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में पहला कन्या विद्यालय खोला। वे दलितों और महिलाओं की शिक्षा के बड़े पैरोकार थे।
स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के माध्यम से शिक्षा का प्रचार किया, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित किया।
महात्मा ज्योतिराव फुले पिछड़े वर्ग और स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत रहे।
महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा (नयी तालीम) का विचार दिया जिसमें काम और शिक्षा को जोड़ा गया।
रवींद्रनाथ टैगोर ने शांतिनिकेतन (विश्व-भारती विश्वविद्यालय) की स्थापना कर वैकल्पिक और रचनात्मक शिक्षा को बढ़ावा दिया।
सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज में शिक्षा सुधार के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखी।गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य बनाने की दिशा में आंदोलन चलाया।
स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का प्रचार
स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के प्रचार को लेकर चले जन आंदोलन में डॉ. भीमराव आंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक समानता का हथियार बताया और संविधान में शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया।महात्मा गांधी की प्रेरणा ग्रामीण शिक्षा और स्वावलंबन पर जोर से कई शिक्षण संस्थानों का निर्माण हुआ।
सरकारी पहलें
1968, 1986 और 1992 की शिक्षा नीतियां, 2009 में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम।
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने बच्चों और युवाओं को विज्ञान व तकनीक से जोड़ने और 'ज्ञान समाज' का विचार देने में प्रमुख भूमिका निभाई। कुल मिलाकर, भारत में शिक्षा के प्रचार की पहल समाज सुधारकों, स्वतंत्रता सेनानियों, धार्मिक-सामाजिक आंदोलनों और सरकार सभी ने मिलकर की। कुल मिलाकर विश्व साक्षरता दिवस हमें यह संदेश देता है कि शिक्षा किसी का उपकार नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का अधिकार है। यह केवल सरकार या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी भी है। जब एक दीपक जलता है, तो उससे दूसरे दीप भी जलते हैं और धीरे-धीरे अंधकार मिट जाता है। ठीक वैसे ही हमारी छोटी-छोटी कोशिशें भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं।
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!