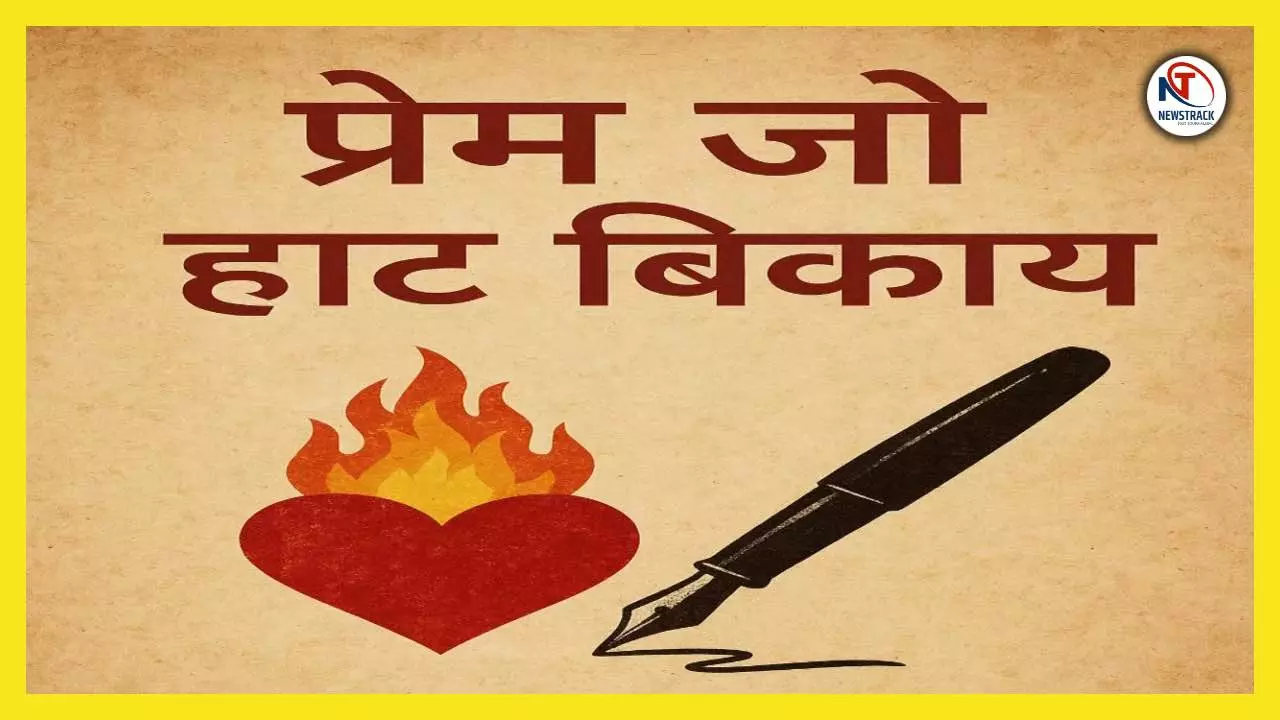TRENDING TAGS :
प्रेम जो हाट बिकाय
Vedas as First Written History: इस लेख में वह आत्मीयता है, जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है।
Vedas as First Written History (Photo - Social Media)
Vedas as First Written History: तेजस्विनावधीतमस्तु। हमारा ज्ञान तेजवान बने। इस वैदिक ऋचा के साथ आरंभ करते हुए विद्ययामृतमश्नुते, मैं कहना चाहूंगा कि इस ज्ञान से अमृततत्व की प्राप्ति हो। कहते हैं कि सृष्टि का आदि ग्रंथ वेद है। विकास क्रम के इतिहास में जहां से सबसे पहले लिखित इतिहास आया वह वेद है। यह भी कहा जाता है कि वेद देव स्तुति से भरे हैं। चूंकि मैंने वेद नहीं पढ़े हैं, इसलिए मान लेता हूं कि ऐसा होगा। लेकिन आज भी इस परंपरा को सूक्ष्म रूप से हम ढो रहे हैं। चाहे कोई आयोजन हो, कार्य की नई शुरुआत हो या लेखन की शुरुआत, हम सर्वप्रथम देव आराधना करते हैं। और वेद तो सृष्टि के आरंभ के दौर का पहला इतिहास हैं, उसमें यदि ऐसा हुआ तो कुछ गलत नहीं हुआ। वेदों में सर्वाधिक प्रार्थना इंद्र की हुई है। इंद्र कौन हैं?अपनी इंद्रियों को यदि हम वश में कर लेते हैं तो हम इंद्र हैं।
इंद्र के बाद सबसे ज्यादा मंत्र अग्नि पर हैं। जरा सी असावधानी पर अग्नि प्रलय मचा देती है। अग्नि से तो हम आज भी डरते हैं। यहां मैं यह नहीं कह रहा कि किस पर कितनी ऋचाएं लिखी गई हैं। सवाल यह है कि ऋचाओं में क्या लिखा गया। बहुत से ऋषियों ने खुद पर ही ऋचाएं लिखी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तात्कालिक समाज के अनुभव का संग्रह हैं-वेद। जो देवों -मनुष्यों ऋषियों के आपसी व्यवहार को व्यक्त या परिभाषित करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम आप आज के युग में एक-दूसरे के प्रति जो विचार रखते हैं, उसे लेखों, पुस्तकों, वाट्सएप, फेसबुक आदि पर शेयर करते रहते हैं। वस्तुतः समाज एक द्वंद्व से आगे बढ़ा है। विभिन्न समाजों के बीच के टकराव से जो रास्ते निकलते गए, वह वेद का अंग बनते गए। पुराने समाज को नए समाज ने राक्षस की संज्ञा दे दी। जैसे आज भी पूर्ववर्ती शासक में हमें इतनी कमियां नजर आती हैं कि हम उसे विलेन बनाकर खड़ा कर देते हैं। विकास यात्रा में जो व्यक्ति या वस्तु सहायक दिखते हैं। हम उसे अपने साथ लाने के लिए आतुर हो उठते हैं। यह प्रवृत्ति स्त्री-पुरुष दोनों में रहती है। पूजा-प्रेम घृणा क्रूरता सभी भावों की अभिव्यक्तियां हमें अपने आसपास दिखती हैं।
वेदों की विशेषता यह है कि वेद में हर ऋचा को रचने वाले ऋषि का नाम दर्ज है। इसे उस काल की ईमानदारी भी कह सकते हैं। वेद की ऋचाओं के रचनाकारों में अनेक स्त्रियां हैं। इसीलिए सबका नाम उनकी रचना के साथ दे दिया गया है, ऐसा मुझे लगता है। हर युग में मनुष्य के आचार, धर्म आदि बदलते रहते हैं। फिर इतिहास का क्या काम ? दरअसल, यह हमें उस युग के लोगों के आचार व्यवहार का ज्ञान कराता है। कहां गलतियां हुईं, उसे बताता है, ताकि जो गलती हुई हैं उन्हें दोहराने से नई पीढ़ी बच सके। प्रकृति आज भी हमें ऊर्जा देती है और याचक हम आज भी हैं।कामनाएं जो तब र्थी वही आज भी है, बस उनका स्वरूप बदल गया है।मतलब ब्रह्म वाक्य जैसा कुछ नहीं।
आज के दौर में हमसे पहले जो लेखक हुए यदि हम उनका स्मरण रखते हैं, तब यह तो नहीं कहा जा सकता कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है।अनुभवों को स्वान्तः सुखाय लिख लीजिए। अब यह कल्पना है, तो अच्छी कल्पना है कि जब कुछ नहीं था तब शिव थे। यथा शिवत्व को पाने की लालसा हर इंसान में करोड़ों दुर्गुणों के बाद भी होती है।
मैं सोचता हूं कि मनुष्य क्या है या कौन है, तो समझ में यह आता है कि मानस ही मनुष्य है, अर्थात मनुष्य का चित्त, उसका मन ही मनुष्य है। सारे संयम मन से ही संचालित होते हैं। कबीर ने भी लिखा है "मन ना रंगाये रंगाये जोगी कपड़ा।" मन यानी मानस में अनुभव व अनुभूतियों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही विद्या है, वही बुद्धि है और उसे ही श्रेष्ठ कहा गया है।
मेरे जीवन की यात्रा साधारण परिवेश से शुरू हुई थी। लेकिन भीतर कहीं यह विश्वास पलता रहा कि शब्द दुनिया बदल सकते हैं। पत्रकारिता ने मुझे उस विश्वास को जीने का अवसर दिया। जब पहली बार अख़बार में मेरा लेख छपा, तब लगा कि मेरी आवाज़ अब मेरी नहीं रही, यह समाज की आवाज़ बन गई है। लेखन मेरे लिए कभी केवल शौक़ नहीं रहा, न ही यह केवल आजीविका का साधन बना। यह मेरे लिए एक जीवन-दृष्टि है, एक ऐसा सेतु है जिसके सहारे मैं समाज से, समय से और स्वयं से निरंतर संवाद करता आया हूँ।
जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि कलम ने मुझे उसी तरह आकार दिया है जैसे नदी अपने किनारों को तराशती है। मैंने शब्दों के माध्यम से न केवल घटनाएँ दर्ज की हैं, बल्कि उन घटनाओं के पीछे छिपे दुख, पीड़ा, संघर्ष और आशाओं को भी जीवंत करने का प्रयास किया है। कभी मैंने किसानों की व्यथा सुनी, कभी मज़दूरों की पुकार। कभी मैंने सत्ता की नृशंसता देखी, तो कभी समाज की संवेदनहीनता। इन सबको लिखते समय मैं हमेशा यही सोचता रहा—“अगर मैं न लिखूँ तो इन आवाज़ों को कौन सुनेगा?”
मेरे पूर्ववर्ती संकलनों—‘समय पर’, ‘शब्द पथ’,’समय के सवाल’, ‘समय के आलेख’, ‘काल प्रवाह’, ‘कालचक्र’— सब इसी प्रश्न और इसी जिज्ञासा के विस्तार हैं। प्रत्येक पुस्तक में मैंने समय के साथ संवाद करने का प्रयत्न किया है। समय से मुठभेड़ करना, उसके प्रश्नों का उत्तर खोजना और उसके संकेतों को समझना ही मेरी लेखनी का मूल प्रयोजन रहा है।इन पुस्तकों में कहीं राजनीति की गूंज है, कहीं समाज की पीड़ा, कहीं संस्कृति की आत्मा। ये केवल लेखों का संग्रह नहीं हैं, बल्कि मेरे जीवन के वे पड़ाव हैं जहाँ मैंने ठहरकर समाज के चेहरे को पढ़ा और फिर उसे शब्दों में ढाला।इन लेखों में राजनीति भी है, समाज भी है, संस्कृति भी है और संवेदनाओं का संसार भी। कहीं मेरी बेचैनी है, कहीं मेरी उम्मीदें हैं, और कहीं वह ज़िद भी है कि समाज बदल सकता है।
मेरे द्वारा इन विचारों की स्थापना के मूल में सामाजिक चेतना का भाव है, परिवर्तन की माँग है? इस वर्तमान भौतिकवादी युग में, किस्तों में जिंदगी जीता, आदमी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दिनों दिन मशीन बनता जा रहा है। वह समय का बहुत ही चालाकी से व्यापार कर रहा है। सच यह भी है कि जब दुनिया में समय की कलाबाजी हो रही है, कोई भी अपना समय निःस्वार्थनष्ट नहीं करना चाहता। मैंने भी अपना समय नष्ट नहीं किया है। सदियों से या जब से साहित्य का आविर्भाव हुआ उसको सदानीरा शाश्वत माना गया है। उसका प्रवाह नहीं रुकता। यह जरूर होता है कि कालक्रम के अनुसार उसका रुख परिवर्तित होता रहता है। कई बार भाव की अभिव्यक्ति के तत्कालीन स्थितियों से प्रभावित होने की गुंजाइश रहती है।
जब हम किसी विषय पर कुछ भी लिखते हैं, तो हमारा वह लेखन, हमारे ज्ञान को दर्शाता है। इस विश्व में जितना भी लिंकित साहित्य है, वह मन की बात है। और मन निरन्तर परिष्कृत होता जाता है।जो कुछ भी हम लिखते हैं, भले ही उस दौर की हमारी पीड़ा हो या खुशी।रुचिकर हो, या अरुचिकर। कह सकते हैं कि लिखते समय वह मन को भाया इसलिए लिखा।
मैं भी आज कुछ इसी पीड़ा या सृजन की प्रक्रिया से गुजर रहा हूं। इस किताब में चाहे कबीर और गांधी की समानता पर मेरे विचार हों याअंत्योदयी समाजवाद पर नरेंद्र देव, डॉ. राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाशनारायण, पं. दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दृष्टि में एकलय देखने का मेरा नज़रिया, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक ही हार में गुथें हुए पंच देव थे, ये महापुरुष। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसमें प्रत्येक जन अपने लिए उचित अनुचित का फैसला करने का अधिकार किसी दूसरे को न देकर खुद लेता है। उत्सव मन की उस अवस्था का आईना या पैरामीटर है जो हमे अगले दिन के लिए जीवन शक्ति देता है। जीवन से लेकर मृत्यु तक एक उत्सव है और यह उत्सव हमारी आगे की मंज़िल हासिल करने की सीढ़ी है।
जिंदगी क्यों बोझ बन रही है उस अवस्था का चित्रण है।खिचड़ी पुराण है। लोकतंत्र से लोक के गायब होने की चिंता और हाट मेंप्रेम के बिकने का दुख है। बुराई का प्रतीक रावण ही क्यों है यह पीढ़ियों से सवाल है। अपने नज़रिये से योगी के कार्यातरण, तुलसी, कबीर, कलाम, पं. दीनदयाल उपाध्याय और पं. मदनमोहन मालवीय को देखने की कोशिश है। प्रेम को समझने और समझाने का प्रयास है। प्रेम के योग और भोग का चित्र है। उत्सव, मौत, मशीन से मुकाबिल आदमी तथामशीन होता आदमी, वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद तथा हाईवे जैसे सवालों पर मेरी सोच, समस्याएं और फिर उनको लेकर उरज रही दुश्चिंताएँ शायद आपको भी परेशान करें। धर्म को हथियार और ढाल बनाने की कोशिश भी शायद आपके लिए हमारे जैसी ही चिंता का सबब हो ।
एक स्वतंत्र व्यक्ति ही निर्भीक व सचेत रह सकता है। निर्भीकता मनुष्य को सामाजिक विद्रूपताओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती है। चेतना दायित्व को समझने में सक्षम बनाती है। स्वावलम्बी बनने की तर्कबुद्धि प्रदान करती है। यहां पर लिखने की स्वतंत्रता मुझे सामाजिक दायित्व में बाधक प्रतीत न होकर सहायक सिद्ध होती है।संवेदनाओं को स्वीकृति प्रदान करते हुए मैं व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों के निषेध को उचित नहीं मानता। कई नयी-पुरानी चुनौतियां औरनुकीले सवाल हमारे आपके सामने हैं। इन पर बहुत ईमानदारी के साथ विचार-विश्लेषण और चिंतन के साथ ही आत्मावलोकन करने के बाद व्यावहारिक घरातल पर मुझे लगा कि हम विसंगतियों एवं विद्रूपताओं के भँवर में फंसे हैं। व्यवस्था की विद्रूपताओं पर चोट करते समय मुझे थोड़ा बहुत भी संकोच या हिचकिचाहट नहीं हुई।
मेरे लेखों में राजनीति है, पर वह नितांत राजनीतिक नहीं; समाज है, पर वह सूखा समाजशास्त्र नहीं; संस्कृति है, पर वह केवल लोकाचार नहीं। इन सबके बीच में वह आत्मीयता है, जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है।मैंने हमेशा यह माना है कि लेखन केवल सूचना देने का नहीं, बल्कि संवेदना जगाने का माध्यम है। यही कारण है कि मेरे लेखों में कभी-कभी इतिहास बोल उठता है, कभी मिथक, कभी गाँव की चौपाल, तो कभी संसद का कोलाहल। पर इन सबमें जो तत्व निरंतर है, वह है—मनुष्य के पक्ष में खड़े होने की जिद।
यह पुस्तक मेरे लिए डायरी भी है और दस्तावेज़ भी। डायरी इसलिए कि इसमें मेरी निजी संवेदनाएँ हैं, और दस्तावेज़ इसलिए कि इसमें समय की गवाही दर्ज है। इसी के साथ मेरे लिए लेखन समाज की जवाबदेही है। यही कारण है कि मैं आज भी कलम को एक संघर्ष का औज़ार भी मानता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक पाठकों को केवल जानकारी ही नहीं देगी, बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर करेगी, संवेदना से भर देगी और उनके मन में यह प्रश्न जगाएगी—“हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है?”
इन्हीं समसामयिक चिंताओं को अपने लेखन में उतारकर आगाह करने के साथ-साथ एक राह पर चलने का आमंत्रण भी दे रहा हूं।यह अलग बात है कि मेरा आमंत्रण कितना स्वीकार होताहै।
इसी विश्वास और इसी उम्मीद के साथ मैं यह संकलन आपके हाथों में सौंप रहा हूँ।
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!